निधि सक्सेना युवा चित्रकार-शिल्पकार, स्क्रीनराइटर और स्तंभकार हैं। लॉस एंजेलिस फ़िल्म इंस्टीट्यूट से फ़िल्ममेकिंग और फ़िल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण लिया है। फ़िल्म डिवीज़न के लिए डॉक्यूमेंट्री व जयपुर दूरदर्शन के लिए टीवी शृंखला- "राग रेगिस्तानी' का निर्माण-निर्देशन। इन दिनों मुंबई में निवास। निधि ने हाल ही में एक फिल्म का निर्देशन किया है।
(भाग-7) विडम्बना देखिए ...ऋत्विक का घर, ऋत्विक के घाट जहां रह गए थे, वो कुछ दिन पहले उसका देस था और राजनीति की दीवारों ने वह भूमि जो कल तक के संघर्षों में अपनी साथी थी- एक थी, उसे इतना पराया कर दिया कि ऋत्विक खुद तो वहां नहीं ही जा पाए, उनकी फ़िल्में, उनकी ये आवाज़ें तक उस पार नहीं सुनाई पड़ीं। ऋत्विक की ये फ़िल्में जिन दिनों पर्दे पर आईं, पाकिस्तान में फ़िल्में प्रतिबंधित थीं, सो ना तो वे ही जा पाए अपना देस, न पहुंचा पाए दृश्यों-आवाज़ों में बंधे अपने ये ख़त, अपने घर तक।
लेकिन हां, ऋत्विक ने इस आज़ादी का मोल चुकाती ज़िंदगियों की कहानी कही कई रूपों में… कुछ लोग उधर थे इन जख्मों को झेलते, कुछ लोग इधर थे, जिन्हें ये दर्द सालते थे और कुछ दोनों तरफ के, जो मानवता के इन भीषण दागों पर चुपके-चुपके आंसू थे और इन लोगों के मन का इन फ़िल्मों ने, इन फ़िल्मों साथ इन धड़कनों ने दिया।
नन्हे-नन्हे ज़ख्मों के बड़े दाग
अपनी फ़िल्मों में ऋत्विक ने कहीं क्रांति के बड़े-बड़े महल नहीं सजाए, भाषणों के जुमले नहीं उड़ाए, खून से लबरेज़ होलियां नहीं दिखाईं, छोटी-छोटी बातें कीं-नन्हे-नन्हे ज़ख्मों की, उस पीड़ा की, जो दिखती नहीं, लेकिन हर दिल को दागी ज़ख्म बन सालती हैं। ये ऋत्विक की आपबीती थी...अपने घर, धरती, मिट्टी, पेड़ों, नदियों से अलग अनजान जगह पे इतनी दूर चले आने की नियति की। पीछे कोई राह तक नहीं, जिस पे मुड़ के फिर घर का दरवाज़ा मिलता हो।
यह भी पढ़ें : दोस्त ने राजेश खन्ना के मुंह पर कह दिया- 'छोड़ ना चौकीदार से क्या बात करनी!'
इस बंटवारे ने मासूम ऋत्विक की जड़ें तो उखाड़ दीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मिट्टी को हर जगह बयां किया। समझने वाला कोई संवेदनशील मन हो तो एक बच्चे के मन की ये तस्वीरे बयां कर देंगी विस्थापन की भयावहता। ऋत्विक घटक खुद मानते थे कि कला को खूबसूरत होना चाहिए मगर उससे भी पहले कला को सच्चा होना चाहिए और ये सच, कोई शाश्वत सच नहीं है। हर कलाकार को एक दर्द भरी निजी प्रक्रिया से गुजरकर अपने निजी सत्य को जानना होता है, यही उसे सम्प्रेषित करना होता है।
कैसे हाथ आए मन के ये सच-हां कहानी तो मन ही में रखी होती है, फिर भी कभी मिलती नहीं है। किसी को कहीं मिल जाती है। ठीक वैसे, जैसे कोई अपनी बात जोर-शोर से कहता है और कोई खूब-खूब कहना चाहता है और कहने की हिम्मत नहीं...या बात को शब्द नहीं, शब्द को आवाज़ नहीं मिलती। पर ऋत्विक तो कह रहे थे, खूब-खूब कह रहे थे और ना सिर्फ कह रहे थे, सारी विपरीत परिस्थितियों को पछाड़ के कह रहे थे। क्या था उनके दिमाग में? हां, वे यह कहते थे-एक काश्तकार और एक ब्राह्मण मिलकर ही कुछ बना सकते हैं और मुझमें वो दोनों हैं।
वो गुस्सा भी हो जाते थे, कहते थे- 'Films are not made thay built'. जैसे- इमारत खड़ी होती है, ना एक-एक ईंट रखकर, उसी तरह फ़िल्म बनती है। शॉट दर शॉट जोड़ा जाता है। ऋत्विक दा का कहने को बेकरार मन और हुनरमंद मानस रच देता था चलती-फिरती करतीं तस्वीरें, ऐसे ही बनी अजांत्रिक।
कुमार साहनी और ऋत्विक दा हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, एक फ़िल्म बार-बार चलाते हैं और फिर, फिर उतने ही बेकाबू होकर हंसते हैं। वे देख रहे थे दुनिया की पहली फ़िल्म, 1896 में बनी, ल्युमेर ब्रदर्स की एराइवल ऑफ ए ट्रेन एट Ciotat स्टेशन. हां, इस फ़िल्म ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई थी…कमरे में, परदे पर चलती ट्रेन देख लोग डर गए। ये ट्रेन आकर सीधा हमसे ही भिड़ेगी।
पहली-पहली बार खूब भगदड़ मची, पर ये ऋत्विक घटक क्या सोच रहे हैं। वे कहते थे- 'मुझे हंसी आई कि देखो एक मशीन दूसरी मशीन को देख रही है। ऋत्विक ने सोचा होगा, वाह अगर मशीन-मशीन के मिलाप से यूं जादू होता है, तब मानव और मशीन मिलकर क्या असर करेंगे, देखें और बन आई, छा गई फिल्म अजांत्रिक सिने पटल पर।'
एक बार उनसे किसी ने पूछा आनेवाली फ़िल्मों के बारे में, तब उन्होंने बताया कि अस्पताल की ऊबी फिज़ा में अखबार के धूसर पन्नों पर उन्हें एक बीमार खबर मिली। एक गांव की लड़की बिशनुप्रिया के wagon brekars काले साए से लग गए और तब तक लगे रहे, जब तक उन पांचों ने उसे धर नहीं दबोचा। उस सौंदर्य ने उन्हें बहकाने की कोशिश में कहा भी कि साड़ी बदलकर, कुछ सज-कुछ निखरकर आती हूं और बहाने के सहारे भागी भी, लेकिन हाथ आई और ऐसा आई कि जंगल के बीचोबीच उन दरिंदों का शिकार हो गई। सत्ययुग अख़बार के युवक पत्रकार ने उसे बचाना भी चाहा, लेकिन बिशनुप्रिया पर मिट्टी का तेल डाल राख बना दिया गया। वो गरीब ब्राह्मण की बेटी न गांव छोड़ सकती थी, ना जीवन, लेकिन अंत ज़िंदगी की जुदाई ही में हुआ। ऋत्विक दा का मन रो रहा था, चेहरा गुमसुम, फिर कहा- इस सत्य वारदात की रपट फ़िल्म में लिखूंगा। स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। मुझे ये ख़बर विस्थापन के दिनों की याद दिला गई।
यह भी पढ़ें : नसीर साहब ने इरफान से कहा- 'अपनी अम्मी को कहना मैं इतना बुरा भी नहीं!'
ऋत्विक कहते थे- बंगाल में किसी गांव में भी चले जाइए, हर डगर पर कहानी मिलेगी, हर घर में कोई गाता होगा- "सची माता गो, आमी जुगे-जुगे होई जनोमो दुखिनी"। यूं, फ़िल्मकार बड़े साहित्यिक प्राणी होते थे पर अपनी कहानियां ऐसे चुनते थे ऋत्विक जीवन से। हां, साहित्य की बात करते तो थे, लेकिन दिव्य नहीं, बड़ी कड़वी-कड़वी।कहते थे बंगला में बहुत संवेदनशील लोग हैं समझदार और असली बुद्धिजीवी, एक नहीं सैकड़ों हैं। किसी भी नदिया किनारे चले जाओ, लोग बहस में डूबे व्यस्त होंगे, लेकिन रचनाकार/ लेखक? बंगला में अब कोई भी जेनुइन लेखक नहीं! लेखन जो हो रहा है, वो वास्तविक नहीं, वे सिर्फ अपने नाम की खेती करना चाहते हैं। बीज, जड़ अन्न की किसी को चिंता नहीं। केवल लिजलिजी भावनाओं की भयंकर बाढ़ आ गई है साहित्य में, जिन्हें औंधे लेट तकिए के सहारे पढ़ा जा रहा है। ...लेकिन हां, कुछ हुए हैं अपनी बंगला माटी में, जो सच में साहित्य निधि हैं। जिन्होंने सच में लिखकर अमूल्य योगदान दिया है, न केवल साहित्य में, बल्कि हमारे इतिहास और जीवन में भी। वे केवल चार ऐसे उपन्यास पाते थे, जो सही और सच हैं । मणिकबाबू का पुतुल नाचेर इतिकथा, रबीबाबू का चतुरंगा, बंकिम चंद्र का राजसिंहा और गणदेवता।
उनका स्वप्न था इन उपन्यासों को सिने आकार, सिने आवाज़ में ढालना, लेकिन स्वप्नों को तामीर देने के लिए कला के आलावा जो कौशल ज़रूरी है, उसमें ऋत्विक कभी जीत गए, कभी जीत न पाए।
ऋत्विक की फिल्मों के नायक नायिकाएं समाज के बेदखल शक्तिहीन प्राणी थे, जिनके लिए विकास से कहीं महत्वपूर्ण बने रहना था। वे किन्ही सुन्दर स्वप्नों का प्रतिनिधित्व करते, जीतते शक्तिशाली महानायक नहीं थे। यूं सिनेमा का आर्थिक अधार पूरी तरह नायक-नायिका और उनके महानायकत्व पर ही टिका होता है, तब ऐसे साधारण-मामूली वर्ग के लोगों और उनकी आपबीतियों पर कौन पैसा लगाता! ऋत्विक कहते थे- फिल्म पूरी तरह पूंजी आधारित व्यवसाय है। मेरे तकनीशियन, अदाकार, कामगार तो एक-एक फ़िल्म के लिए जान तक लगा देते हैं, मेरे लिए चुनौती फ़िल्म के लिए पैसा लाना है। ये दिक्कत हमारे सामाजिक ढांचे में बढ़ती ही जाएगी और यह सिर्फ फ़िल्म ही की बात नहीं है। क्योंकि लगभग सारे ही पैसे का भाव काले बाज़ार की ओर है।
Read This Also : EVERY ART IS POLITICAL!
हमारे देश का 11 हजार करोड़ सफ़ेद धन के रूप में घूम रहा है तो 33 हजार करोड़ काले बाज़ार में हैं। दरसल, बेईमानी करने वाले डाकुओं के पास ही कैश है और वे या तो हिस्सा हैं इस तन्त्र का या वे खुद, जो देश तंत्र चला रहे हैं। सरकार ये बात मानती है कि अर्थव्यवस्था पर काले बाज़ार ही का कब्जा है। दरअसल, यहां 1 रुपए का असली मूल्य 25 पैसा ही रह गया है और बहुत जल्दी इस सबकी पोल खुल जाने वाली है। जल्दी ही यह सब खुल कर सामने आ जाएगा, जब महंगाई के कारण लोग खाना भी नही पाएंगे और उस अकाल में इस व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। देखिएगा 100 साल के भीतर रोटी के लिए विशाल गृहयुद्ध खड़ा हो जाएगा। फ़िल्म तो इस सबका बहुत छोटा हिस्सा है। ज़रूरी है कि निडर हो के बोलें। व्यक्त करें, विरोध करें, लेकिन लगता है ये बुद्धिजीवी कुछ करेंगे नहीं। ये बहुत रीढ़ विहीन हो चले हैं। ऋत्विक दा कभी चिल्लाते थे- "I have survived …I survived!"

पहला भाग : बिछड़े घर की तलाश में उम्र भर सफ़र
दूसरा भाग : मुझे चिल्लाना है, कहने का मोह है... सुन लो!
तीसरा भाग : प्रोटेस्ट का फॉर्म था सिनेमा, सेल्युलाइड पर चमके सियासी सवाल
चौथा भाग : जिस फिल्म को मेलोड्रामा कहकर 'भारत' ने नकारा, वो वर्ल्ड सिनेमा में बनी कल्ट!
पांचवा भाग : बतौर निर्देशक दो बार नकारे जा चुके थे ऋत्विक घटक, फिर लेकर आये वो फिल्म जो बन गई कल्ट
छठवां भाग : 'वो किरदार कीट्स की कविताओं और आराम कुर्सी के सपने में जीता है!'



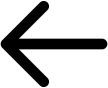 Previous
Previous










.%5B1%5D.jpg)









Leave your comment