पवन कुमार विभिन्न दृश्य माध्यमों के लिए वृत्त-चित्र लेखन, विज्ञापन लेखन, कथा, पटकथा, संवाद लेखन; संगीतकारी व गीतकारी के पुराने खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वो कविता, कहानी अनेक विधाओं में विपुल लेखन करते हैं। कुल मिलाकर वो 'हिलांश' के मूल मिजाज के करीब के लेखक हैं। फिलवक्त उन्होंने अपना आशियाना मुंबई में बनाया हुआ है और यहीं से वह अपनी रचनात्मक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
कहानियां या तो क़िताब का सफ़ेद कागज़ी पैरहन पहन कर आती हैं या फिर फिल्म की रंग-बिरंगी डिजाइनर ड्रेस पहन कर लोगों को आशकारा हुआ करती हैं। मैं कहानी का दिलफेंक महबूब तो हूं, पर मेरा दिल जिनका शैदाई हो जाए, वैसी दिलनवाज़ और पुरकशिश कहानियां मुझे बामुश्किलन ही मिला करती हैं।
अमूमन हलवाई मिठाई का शौकीन नहीं हुआ करता। बहुत सम्भव है कि ख़ुद अफ़सानानिगार होने की वज़ह से मैं भी कहानियों में आसानी से लज्ज़त नहीं पा पाता। शायद इसलिए लफ़्ज़ों के तंग कूचे से गुज़र कर मंटो की मक़बूलियत ढूंढता हूं, तो हाथ कुछ नहीं लगता। शायद इसलिए ख्यातिलब्ध नाम Giuseppe Tornatore की फ़िल्में 'सिनेमापेरेडिसो' या 'मलेना' मुझे महज़ एक ख़ूबसूरत मुसव्विरी (Portrait) तो Quentin Tarantino की बहुचर्चित फ़िल्म 'वन्स अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड' मुझे दार्शनिक पेचीदगियों का अड्डा भर ही लगती हैं। मैं तो अकीरा कुरोसावा की फ़िल्म 'रोशोमन' को भी पुरातन साधनहीनता के मध्य बोया कल्पवृक्ष का बीज कहता हूं, कल्पवृक्ष नहीं।
बड़े नाम भी मेरी महसूसियत की मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाते। इसे मेरी बेअदबी कह दीजिये, पर मेरी पसन्दगी की कहानियों में 'डू एंड डोंट' के सूत्र नहीं होते, सिंथेटिक एलिमेंट नहीं होते, मिथ्यारोपित आदर्शवादिता नहीं होती, व्याकरण नहीं होता, उनमें होता है बस तर्क की गंगोत्री से निर्गमित सदानीरा सरिता सा सतत बहाव। यह भी समझ लीजिए कि मेरे हिसाब का तर्क औचित्य की बस एक कसौटी मांगता है और वह है असम्भव के अंदर का संभाव्य (The Probable Within The Improbable)।अगर आप मुझे संभव के अंदर का असंभाव्य (The Improbable Within The Probable) परोसेंगे, मैं उसे हरगिज़ कहानी नहीं मानूंगा।
यह भी पढ़ें : अच्छी कहानी की 'नब्ज' कहां होती है!

क्या फ़िल्म 'पैरासाइट' ऑस्कर के योग्य थी?
कुछ दिन पहले मैंने इस साल का ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्म 'पैरासाइट' देखी। फ़िल्म की आधी यात्रा तक यूं लगता रहा मानो ऑस्कर ने 'पैरासाइट' फ़िल्म के रूप में बड़ा वाजिब चुनाव किया हो, पर कहानी जैसे ही कॉमेडी का मरहला पार करती है, यह यूं गिरने लगती है जैसे ब्लैकहोल में कोई सितारा।
अचानक से कम्यूनलिज़्म का भूत इसे धर दबोचता है। वर्ग-विद्वेष (Class Rift) जो अब तक संवेदनशीलता के कांख को हौले-हौले गुदगुदाता हुआ कहानी के अवसान की ओर बढ़ रहा था, वही सिलसिलेवारी की आरोही सीढ़ी को झटके से लांघकर अचानक अतिशय वीभत्सता के मुकाम पर जा पहुंचता है। तर्क तो सावन की धूप सा एक बार जो ग़ायब होता है तो पुनः लौटता ही नहीं। यही है सम्भव के अंदर का असम्भाव्य और यही है मेरी नापसंदगी का सबब।
तब फ़िल्म 'द डिक्टेटर' क्यों!
अब बात अपनी पसन्दगी की करता हूं। हालिया मैंने एक फ़िल्म देखी 'द डिक्टेटर'। सन् 2012 में प्रदर्शित हुई इस फ़िल्म के निर्देशक हैं Larry Charles और लेखक हैं Sacha Baron Cohen, Alec Berg, David Mandel और Jeff Schaffer।
दामन पे कोई छींट न ख़ंजर पे कोई दाग़
तुम क़त्ल करो हो कि करामात करो हो
बहुतों ने किसी के बाकमाल हुस्न को मार्रुफ़ शायर कलीम आजिज़ के इस शायरी का सदक़ा दिया होगा, पर मैं यह शायरी वारुंगा फ़िल्म 'द डिक्टेटर' के लिये।क्योंकि इस फ़िल्म ने इस लताफ़त और नफ़ासत से अरब की ख़ुश्क सरज़मीं पर क़ाबिज़ पितृसत्तात्मक और अतिवादी व्यवस्था (Patriarchal and Radical System) का रेज़ा-रेज़ा ऐसे उधेड़ा है कि मक़तूल को इसकी हवा तक न लग पायी है।
आपको ऊपरी नज़र में यह फ़िल्म तर्क से कोसों दूर, किसी बेअक्ल की अहमकाना हरकतों के इर्द-गिर्द बुनी एक सिथेंटिक हास्य पैदा करने वाली फ़िल्म लगेगी पर अगर आप में पंक्तियों के बीच पढ़ने (Reading Between The Lines) का हुनर है, तब आप इस फ़िल्म में मौजूद हंसी-ठठ्ठे के पीछे छिपे, उस मारक तंज़ तक पहुंच पाएंगे जो धर्म के भ्रामक रूप के चाशनी में लिपटा हुये मुखौटा (Sugar Coated Facade) को चकनाचूर करने लिए लिए बहुत ज़रूरी है।
यह भी पढ़ें: चित्रों में महामारी के आंतक का रंग और लॉक डाउन में उलझी कूची की क्रिएटिविटी!
यह फ़िल्म दर्शकों पर कई तरह का तास्सुर छोड़ती है। देखने वाला अगर कट्टर फ़िरक़े का है, तो यह फ़िल्म उसकी हठधर्मिता को बार बार मुंह चिढ़ाती है। यह फ़िल्म कई लिहाज़ से नायाब है। इसका एक अयाना पहलू यह है कि यह फ़िल्म बड़ी आसानी और बेबाकी से बड़ी से बड़ी विवादास्पद बात कह जाती है ।

फ़िल्म के कुछ दृश्यों पर ग़ौर फ़रमाइये!
अमेरिका में सियासती साज़िश का शिकार हो अपनी पहचान और ताक़त खो चुका वाडिया का तानाशाह अलाद्दीन वक़्ती तौर पर मिडिल वाइफ बन एक गर्भवती स्त्री की प्रसूति में मदद करना चाहता है। गर्भवती स्त्री जैसे ही प्रसव के दौरान अपनी टांगे खोलती है, अलाद्दीन भी हस्बे-आदत मुबाशरत (संभोग) करने के लिए अपना पैंट उतारने लगता है!
उसके हाथों जब बच्चा पैदा होता है और जब वह महसूस (Realize) करता है कि बच्चा लड़की है, तो वह बेहिचक बच्चे की माँ से पूछ बैठता है- 'लड़की पैदा हुई है क्या उसे कचरे के डब्बे में फेंक दूं?' कहानी के क्लाइमेक्स में हरीफ़ से शरीफ बन चुके अलाद्दीन की अपनी पत्नी भी जब गर्भवती होती है तो वह अपनी पत्नी को भी स्त्री के प्रति दुराग्रह रखने वाला क्रूर विकल्प देता हुआ पूछता है- 'बेटा पैदा करोगी या गर्भपात करोगी?'
यह उस संसार के औरत विरोधी माहौल का बिना मिलावट वाला विशुद्ध सत्य है। उस दुनिया की जम्हूरियत (Democracy) कितनी स्वांग (Farce) से भरी है, यह फ़िल्म इस सच को भी बड़ी बेबाकी से उधेड़कर सामने रख देती है। तानाशाह अलाद्दीन तानाशाही की निज़ामत तोड़, अपने मुल्क में डेमोक्रेसी का ऐलान कर आवाम को वोटिंग की ताक़त से लैस तो कर देता है, पर उन्हीं वोटर्स की क़तार के आगे टैंक तैनात कर वह उनके मंतव्य को ज़बरन अगवा भी कर लेता है।
पर्दे पर वोटर्स की क़तार के दायीं ओर से आते हुये टैंक की झलक मात्र जब 2 सेकंड से भी कम वक्त में हालिया स्थापित हुई जम्हूरियत को ध्वस्त कर देती है, हमें स्वस्फूर्त अहसास होने लगता है कि उस दुनिया की सच्चाई असल में है कैसी! साथ ही इसी क्षण हमें अहसास होता है, फ़िल्मकार और कहानीकार कितने मेधावीपन से लबरेज अपने काम को अंजाम देने में जुटे रहे।
क्या फ़िल्म पूर्वाग्रह से भरी और स्त्री द्वेषी है?
इस फ़िल्म पर स्त्री द्वेषी (Misogynistic) होने का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है, पर दूसरे नज़रिये से आप इसे पितृसत्तात्मक समाज की नुमाइंदगी करने वाले एक नारीपीड़क (Misogynist) पुरुष अलाद्दीन की ईमानदार और बेबाक कहानी भी कह सकते हैं। ऐसी कहानी जिसने रात को रात कहने से गुरेज़ नहीं किया है।
हां, इस फ़िल्म का नायक (या खलनायक) अलाद्दीन सिर्फ़ वाडिया नाम के एक तसव्वुरी मुल्क का तानाशाह हुक्मरान नहीं है। उसमें आप अरब के चरमपंथियों, यूरोप के फासिस्टों, हिंदुस्तान के धर्मांधों को महसूस सकते हैं। उसकी कारगुज़ारियों में बर्बरता बड़ी मुखरता से जीती है, पर इन्हीं बर्बरताओं के बीच अलाद्दीन कहीं न कहीं यह अहसास भी करा देता है, कि वह मानवीय संवेदिकाओं से सुसज्जित एक आदमी है, जिस पर हालात जनित बेरहमी की एक कठोर परत चढ़ी हुई है। कोई उसकी इस बाहरी परत को किसी तरह चटका दे, तो वह अलाद्दीन के अंदर दबे पिन्हें आदमी तक पहुंच जाएगा। चेतना की अंतिम परत के पीछे छिपा अलाद्दीन का यह प्रच्छन्न स्वभाव एक आश्वासन का प्रतीक (Token Of Assurance) भी है, उन निराशावादियों के लिए जिन्हें ज़मीं के इन हिस्सों के अतिवादियों के साथ सहअस्तित्व बनाये रखना असम्भव लगता है।
यह भी पढ़ें : रंग और रेखाओं के खेल और मेल से उपजी कला का जादू!
'द डिक्टेटर' फ़िल्म एक तरफ़ मुसलमानों के चरमपंथी तबके को बरहना (नंगी) करती है, तो दूसरी तरफ़ वह मुसलमानों के प्रति दुराग्रह रखने वाली पश्चिमी सोच और मिडिल ईस्ट के तेल भंडार (Oil Resoviors) पर गिद्ध दृष्टि रखते मुल्कों की बेशर्म छटपटाहट को भी फ़ाश करती है। नफ़ीस क़िस्म के ही सही पर यूरोप ने भी तानाशाह (Dictator) वाले तेवर समय-समय पर ख़ूब दिखाये ही हैं।
फ़िल्म का आरम्भिक दृश्य है कि तानाशाह अलाद्दीन ने विश्व ओलम्पिक स्पर्धा के तर्ज़ पर अपने अंदाज़ के एक ओलंपिक स्पर्धा का आयोजन किया है, जिसमें वह ख़ुद शिरकत करता है और आगे निकलते एथलीटों को गोली मार अव्वल आता है और सारे मेडल ख़ुद बटोर लेता है। अब इस दृश्य के संदर्भ में ब्रिटेन द्वारा आयोजित किये जाने वाले कॉमनवेल्थ (राष्ट्रमंडल) गेम्स को आंकिये। आपको दोनों में बड़ी रोचक समानता दिखेगी।
इसके लिए आपको कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन के पीछे का अभीष्ट समझना होगा। ब्रिटेन ने बड़ी चालाकी से केवल अपने पूर्वकालिक गुलाम देशों को कॉमनवेल्थ आयोजन में शामिल कर, अपने तत्कालीन साम्राज्य को खेल की आड़ में चिन्हित कर लिया। आज तक यह देश उस दम्भ को, अपने साम्राज्यवादी स्मृति चिन्ह (Imperialistic Souvenir) को पाल पोष रहा है। यहां भी चालाकी, नहीं इसे धूर्तता कहिये... मेडल की तालिका में भारत जब धीरे-धीरे ब्रिटेन को चुनौती देने के क़रीब आने लगा, तो अतीत का यह विश्व अधिपति घबरा गया। उसे लगने लगा कि उसका कभी ग़ुलाम रहा राष्ट्र कहीं उसे ही न पछाड़ दे। इस घबराहट में ब्रिटेन ने तीरंदाज़ी और शूटिंग वो दो खेल, जिसमें भारत की मजबूत स्थिति है, इन्हें कामनवेल्थ गेम से हटा दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसकी जगह ब्रिटेन ने बीच वॉलीबॉल (Beach Vollyball के ऐसे खेल को कॉमनवेल्थ में शामिल कर लिया, जिसे कई भारतीयों ने देखा तक भी नहीं है।

'Live By The Gun Die By The Gun'
अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है 'Those who live by the gun, die by the gun'। बंदूक को क़ायदा मानने वाले तानाशाहों और आतंकवादियों को इस कहावत का सच पता होता है। तभी तो सनक मिजाज़ गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन का ताक़त की मद में अकुलाया बेटा उदय हुसैन, मौत को झांसा देने के लिए इन्होंने अपना बॉडी डबल रखा हुआ था। इनके कई बॉडी डबल्स ने इनके हिस्से की मौत अपने शरीर में खपा ली। 'द डिक्टेटर' फ़िल्म इस ज़ालिमाना तल्ख़ हक़ीक़त को भी बड़े मज़ाकिया अंदाज़ में उजागर करती है।
यह भी पढ़ें - (भाग 1 ) : एक थी काजी, एक था रंगा...!
फ़िल्म का एक दृश्य तो 'जो मरा वह ओसामा बिन लादेन नहीं बल्कि उसका बॉडी डबल था', इस हल्की सी सम्भावना को भी झट से कहकर निकल जाता है। गुदगुदाना और हथौड़े मारना, दोनों क्रिया को साथ-साथ अंजाम देने वाली इस निहायत ही ख़ूबसूरत फ़िल्म को फिल्मों की रोचक रेटिंग वेबसाइट IMDB ने महज़ 6.5 की रेटिंग दी है। ऐसा कर IMDB ने अपने ही हाथों, अपनी आंकलन क्षमता पर सवालिया निशान लगा दिये हैं।
क्या कट्टरता धर्म विशेष की पैदाइश है?
इससे पहले कि अवसरवादी फ़िल्म की मेरी इस विवेचना को आधार बना कट्टरता को धर्म विशेष से जोड़ें, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि धर्म का कट्टरता से कुछ लेना-देना नहीं। कट्टरता विषम भगौलिक परिवेश की पैदाइश है और मेरे इस सोच का पृष्ठांकन करते हैं दो अलग भगौलिक परिस्थितियों वाले ये देश। एक तरफ़ अरब और मिडिल ईस्ट की शुष्क भूमि (Arid Land) पर बसे ईरान, इराक, सीरिया जैसे देश तो दूसरी तरफ़ नील नदी के कछार की उपजाऊ ज़मीन पर बसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और इजिप्ट जैसे देश।
दोनों इलाकों के मुल्कों में एक सा मज़हब है, पर एक इलाके के मुल्कों में बेशुमारियत में खून ख़राबा और अव्यवस्था है, तो दूसरे इलाके के मुल्कों में बेशुमारियत में अमन। इन मुल्कों की निज़ामत में 'इम्तियाज़' पैदा करने वाला कारक आखिर क्या है? वह कारक है खेती बाड़ी और आर्थिक समाजिक उपक्रमों और उद्धमों के लिए आदर्श भगौलिक परिवेश का होना या न होना।
आप खेत को कांधे पर टांग कर घूम नहीं सकते। खेत लोगों को विवश करता है, एक जगह पर सालों टिके रहने के लिए। लोगों का एक दूसरे से सालों तक सरोकार बना रहता है और इसलिए ऐसे इलाकों में एक सौहार्दपूर्ण समाजिक व्यवस्था पनप पाती है। खेती के इर्द-गिर्द एक जटिल अर्थव्यवस्था भी स्वतः पनप जाती है, जिसमें लोग उलझे रहते हैं और इसलिए ऐसे इलाकों में अतिवादिता (Radicalism) कम देखने को मिलती है। इजिप्ट, ट्यूनिशिया, मोरक्को जैसे मुल्क ऐसी व्यवस्था की मिसाल हैं।
इसके उलट रेतीली ऊसर ज़मीन पर जहां खेती सम्भव नहीं हो पाती, लोग यायावर बन यहां-वहां घुमक्कड़ी करते रहते हैं। ऐसे में लोगों का आपसी सामाजिक सरोकार बन नहीं पाता और ऐसे इलाकों में कट्टरवादिता बहुत ज्यादा होती है। अरब और मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर इलाका ऐसे इलाकों का उदाहरण हैं।

भारत के ही सन्दर्भ में कट्टरता को हम ठीक से देखें, तो हम पाएंगे इसे राजस्थान की रेतीली ज़मीन की एक खानाबदोश जनजाति पारधी की रिवायतों और संस्कारों में प्रश्रय पाते हुये। यह पारधी जनजाति 'कच्छा-बनियान गिरोह' के नाम से भी बड़ा कुख्यात है। इनका धर्म है लूटना। इनके संस्कार का हिस्सा है लूटकर पीड़ित को जान से मार देना। ये अपने बर्बरतापूर्ण कार्य को अंजाम देने से पहले मां कलिका की पूजा करते हैं। राजस्थान से उद्गमित यह जनजाति आज की तारीख़ में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश तक फैली हुई है। इन जगहों में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों सी दुश्वारियां नहीं, पर लम्बी कंडीशनिंग ने नये इलाकों में भी इनकी आपराधिक मनोवृत्ति की जड़ता बरक़रार रखी है।
कंडीशनिंग बड़ी जब्बर चीज़ होती है, जो डीएनए में घुलकर कई संततियों तक चिपकी रहती है। इसे तोड़ने की दो तरकीबें हैं। एक, उन तमाम गुरुओं और तालीमों से सम्बंध विच्छेद जो व्यक्ति और बरगलाने वाली पुरातन परम्पराओं के बीच सेतु का काम करते हैं। दूसरी तरक़ीब है, अभिनव और अन्वेषणात्मक सोच को अपनाना। इसे ही डी-रैडिकलाइजेशन (Deradicalization) या लिबरेलाइजेशन (Liberalization) कहते हैं।
फिलहाल इतना ही, अगली कड़ी में कहानियों की बातें लेकर हाजिर होता हूं...
(जारी है...)



.jpg)







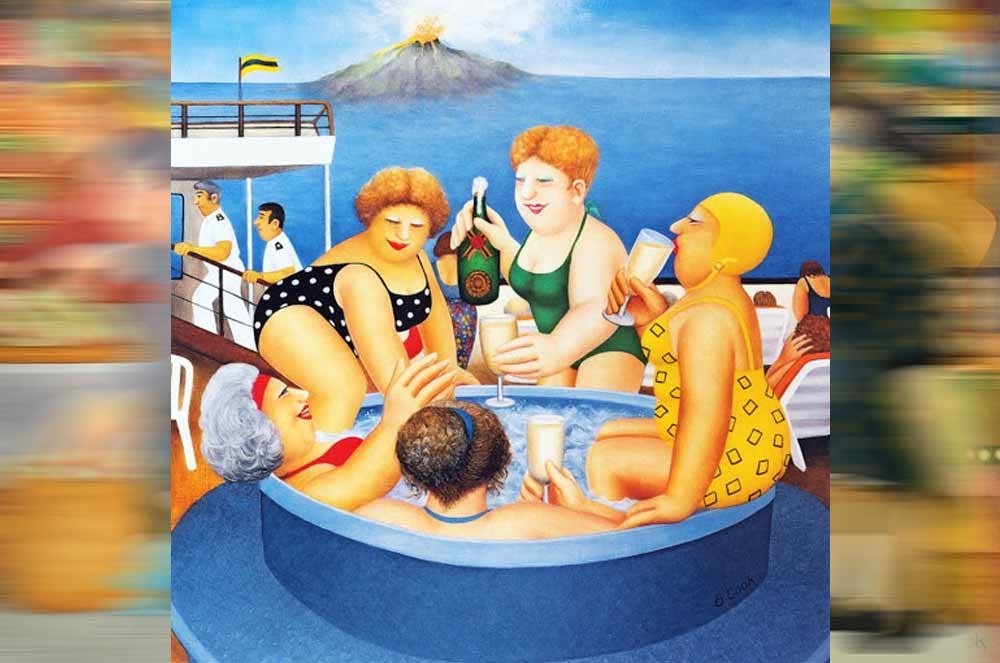

.%5B1%5D.jpg)









Leave your comment