अजीत राय को हम सीनियर कल्चर जर्नलिस्ट और आर्ट क्रिटिक बतौर भी जानते हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मीडिया टीचर के बतौर भी। मुख्यधारा के मीडिया में जब सिनेमा पर सतही रपट नजर आती हैं, तब अजीत हमें सिनेमा की दूसरी दुनिया से परिचित करवाते हैं। वो सही मायनों में सिनेमा को बारीकी से जानते हैं।
अफगानिस्तान के बारे में इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। वहां तालिबान का कब्जा हो चुका है और सारी दुनिया अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान के सिनेमा के बारे में दुनिया भर में बहुत कम चर्चा होती है। आश्चर्य है कि भारत में भी इस बारे में कभी कोई खास बातचीत नहीं सुनी गई है, जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं। रवींद्र नाथ टैगोर की कहानी 'काबुलीवाला' पर पहले बंगाली में साल 1957 में तपन सिन्हा और बाद में हिंदी में साल 1961 में हेमेन गुप्ता सहित कई भारतीय निर्देशकों ने सफल फिल्में बनाई हैं।
अफगानिस्तान में साल 2007 में आई हालीवुड की 'द काइट रनर' से लेकर साल 1975 में आई फिरोज खान की फिल्म 'धर्मात्मा', साल 1992 में मुकुल आनंद की फिल्म 'खुदा गवाह', साल 2006 में आई कबीर खान की फिल्म 'काबुल एक्सप्रेस' समेत कई फिल्में बनती रही हैं। हालांकि, अफगानिस्तान में बनने वाली भारतीय फिल्में अपनी पटकथा के चलते कभी उतनी अच्छी नहीं बनी, जिससे उनकी व्यापक तौर पर चर्चा हो सके।
अफगानिस्तान में सिनेमा को लाने का श्रेय वहां के राजा (अमीर) हबीबुल्ला खान को जाता है, जिन्होंने साल 1901-1919 के दौरान सबसे पहले राज दरबार में प्रोजेक्टर से कुछ फिल्में दिखाई थी। प्रोजेक्टर को तब वहां 'जादुई लालटेन' कहा जाता था। हालांकि, यहां सिनेमा की पहुंच तब के एलीट तक ही बरकरार थी और काफी सालों बाद साल 1923 में आम जनता के लिए काबुल के पास पघमान शहर में एक मूक फिल्म के प्रदर्शन का जिक्र मिलता है। पहली अफगान फिल्म साल 1946 में बनी थी, जिसका नाम था 'लव एंड फ्रेंडशिप'। उसके बाद वहां अधिकतर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती रही, जिसे भारत से आई फीचर फिल्मों से पहले दिखाया जाता था। अफगान सिनेमा में वीरानी पसरने जा रही थी। साल 1990 में गृह युद्ध और उसके बाद साल 1996 में तालिबान के सत्ता में आते ही अफगानिस्तान में सिनेमा बनाना और देखना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वो दौर था, जब अफगानों का भविष्य उस अंधेरी सुरंग में धंस गया था, जहां सिर्फ मायूसी और कड़े धार्मिक प्रतिबंध ही नजर आते थे। लोंकतंत्र से दूर जब अफगानिस्तान की संपदा को लूटा जा रहा था, तब इस सब पर सवाल उठाना बंद था... सिनेमा बनाना बंद था।
विश्व सिनेमा में यहां की फिल्मों की चर्चा तब शुरू हुई जब साल 2001 में मशहूर फिल्मकार मोहसिन मखमलबाफ की फिल्म 'कंधार' दुनिया भर के करीब बीस से अधिक फिल्म समारोहों में दिखाई गई। इस फिल्म ने पहली बार एक लगभग भुला दिए जा चुके देश की गुमनामी से निकलकर अफगानिस्तान की ओर दोबारा दुनियाभर का ध्यान खींचा। बाद में उनकी बेटी की फिल्म 'ऐट फाइव इन द आफ्टरनून' साल 2003 में दुनियाभर में चर्चित हुई। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी अफगान लड़की की है, जो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ स्कूल जाती है और एक दिन अफगानिस्तान की राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देखती है। फिल्म का नाम मशहूर स्पेनिश कवि फेदेरिको गार्सिया लोर्का की कविता के शीर्षक से लिया गया है।

इन संदर्भों से आगे सच्चे अर्थों में यदि किसी अफगानी फिल्म ने विश्व सिनेमा में अब तक सबसे महत्वपूर्ण जगह बनाई है, तो वह है सिद्दिक बर्मक की साल 2003 में आई फिल्म 'ओसामा'। इस फिल्म को न सिर्फ कान फिल्म समारोह समेत दुनियाभर के कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार मिले, बल्कि इस फिल्म ने तकरीबन 39 लाख डॉलर का कारोबार भी किया। फिर इसके ठीक अगले साल आती है अतीक रहीमी की फिल्म 'अर्थ एंड एशेज' जो अफगानिस्तान में खाकेस्तार-ओ-खाक के नाम से प्रदर्शित की गई थी। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 57 वें कान फिल्म समारोह के अन सर्टेन रिगार्ड खंड में हुआ था। इसके बाद जिस फिल्म की चर्चा होती है, वह है ईरानी फिल्मकार वाहिद मौसेन की सााल 2011 में आई फिल्म 'गोल चेहरे'।
यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान की उस फिल्ममेकर का खत, जो महिलाओं के लिए मांग रही है मदद
इस वक्त अमेरिकी और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के चले जाने के बाद उपजे हालातों और सिर्फ काबुल एयरपोर्ट और पंजशीर घाटी के अलावा समूचे प्रांतो पर तालिबान के कब्जे में जाने के बाद से ही अफगानिस्तान लगातार खबरों में बना हुआ है। एक बार फिर से अफगान फिल्मों का काला दौर शुरू हो चुका हैं फिल्म कलाकार डरे हुए हैं। तालिबान ने अफ़गान फिल्म उद्योग को लगभग तहस-नहस कर दिया है। तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध भी चल रहा है। यह देखकर सुखद भी आश्चर्य होता है कि अफगानिस्तान में बनी अधिकतर फिल्में तालिबानी कट्टरपंथी मुस्लिम विचारों के खिलाफ सिनेमाई प्रतिरोध है।
अब सिद्दिक बर्मक की फिल्म 'ओसामा ' को ही ले लीजिए जो कि तालीबानी शासन में एक तेरह साल की लड़की (मरीना गोलबहारी) की कहानी है। मरीना अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए लड़का बनकर काम करती है और अपना नया नाम रख लेती है- 'ओसामा'। उस बच्ची के परिवार में अब कोई मर्द नहीं बचा हुआ है। वह अपनी मां के साथ एक अस्पताल में काम करती थी, जिसे तालिबानियों ने बंद कर दिया और औरतों के घर से बाहर निकल कर काम करने पर रोक लगा दी गई। अब मरीना के सामने संकट है। वे लड़कों को पकड़ कर इस्लामी ट्रेनिंग कैंप भेजने लगे तो एक दिन 'ओसामा' भी पकड़ लिया गया। कैंप में पीरीयड आ जाने से मरीना पकड़ी जाती है। तालिबानी उसे ठंडे कुंए में उल्टा लटका देते हैं। अंततः एक बूढ़े अय्याश शख्स के साथ उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, जिसकी पकी हुई दाढ़ी बतौर इंसान हमपर सवाल उठाती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि गर्म पानी से भरे टैंक में बूढ़ा अय्याश नहा रहा है। टैंक के पानी से भाप उठ रही है और पास में कैद 'ओसामा' डर से थर-थर कांपती हुई सिसक रही है। यह शानदार फिल्म हमें अफगानिस्तान के भीतर औरतों और बाकी लोगों के लिए तालिबानी शासन कैसा होगा, इसकी झलक देती हुई कहीं भीतर तक सिहरन पैदा कर जाती है।

ईरानी फिल्मकार वाहिद मौसेन की साल 2011 में आई 'गोल चेहरे' एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। गोल चेहरे असल में अफगानिस्तान में एक सिनेमाहॉल का नाम था। इस सिनेमाहॉल को जब तालिबानियों ने निशाना बनाया, तब लोगों ने जान पर खेलकर इस हमले से कई दुर्लभ फिल्मों के प्रिंट बचा लिए थे।
फिल्म की कहानी एक उन्मादी सिनेमा प्रेमी अशरफ खान की कहानी दिखाती है, जो गोल चेहरे नाम से एक सिनेमा हॉल चला रहा है। एक रोज तालिबानी सिनेमाहॉल को जलाकर नष्ट कर देते हैं। लोग इस सिनेमा हॉल को दोबारा बसाना चाहते हैं। वे अफगान फिल्म आर्काइव के निदेशक की मदद से बड़ी मुश्किल से ईरान जाकर एक ऐसे आदमी को ले आते हैं, जो फिल्में दिखाने के लिए प्रोजेक्टर लगा सकता है। सत्यजीत राय की फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' के प्रदर्शन से ही सिनेमा हॉल गोल चेहरे का उद्घाटन होता है, लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है, तालिबानी बम से सिनेमा हॉल को उड़ा देते हैं। वे अशरफ खान को मार देते है। वो फिल्म आर्काइव की सभी फिल्मों को जला देने का फतवा जारी करते हैं।
रेड क्रॉस हास्पिटल में काम करने वाली एक विधवा डाक्टर रूखसारा आर्काइव की दुर्लभ फिल्मों को बचाने की योजना बनाती है। तालिबानी दौर के खौफनाक लम्हों में भी रूखसारा हिम्मत नहीं हारती। अमेरिकी फौजों द्वारा तालिबानियों के सफाए के बाद रूखसारा ईरानी सिने जानकार और अफगानी फिल्म आर्काइव के निदेशक की मदद से एक बार फिर गोल चेहरे सिनेमा हॉल का निर्माण करवा देती हैं और सत्यजीत राय की फिल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' के प्रदर्शन से ही इसका उद्घाटन करती हैं। इस फिल्म में अफगानिस्तान में भारतीय फिल्मों के प्रति दीवानगी का आलम देखने को मिलता है।
यह भी पढ़ें: सुपिन मेरे ख्यालों की नदी है, जिसके ऊपर लायबर दौड़ रहा है!
अतीक रहीमी की साल 2004 में आई फिल्म 'अर्थ एंड एशेज' जिसका मूल नाम 'खाकेस्तार- ओ खाक' है, अब्दुल गनी के उम्दा अभिनय के लिए भी देखी जानी चाहिए। इसमें उन्होंने एक बूढ़े का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है- 'अमेरिकी फौजों की बमबारी से तबाह हो चुके अफगानिस्तान में एक बूढ़ा दस्तगीर अपने पोते यासिन के साथ सड़क किनारे बैठा हुआ किसी लंबी यात्रा के दौरान सुस्ता रहा है। यह धूल धूसरित सड़क कोयले की उस खान तक जाती है, जहां दस्तगीर का बेटा काम करता है। बूढ़े दस्तगीर को अपने बेटे के पास पहुंच कर बताना है कि उनका गांव और परिवार बमबारी में नष्ट हो गए हैं। उस बूढ़े दस्तगीर के लिए यह यात्रा मुश्किलों से भरी हुई है। वह असह्य अकेलेपन और मिट्टी में मिल चुके अपने सम्मान के बीच कहीं फंसा हुआ है। इस यात्रा में उसे तरह-तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। इनमें एक विक्षिप्त चौकीदार, दार्शनिक दुकानदार, अंतहीन इंतजार करती रहस्यमयी स्त्री और इस बेमतलब युद्ध से तबाह हुए वो लोग हैं, जो कहीं जा रहे हैं। रात होते ही ठंढ जानलेवा होने लगती है। बूढ़ा दस्तगीर ठंढ से बचने के लिए लकड़ी की उस घोड़ा गाड़ी को ही जलाकर रात गुजारता है, जिसे वो अपने पोते के लिए लाया था। दूसरी सुबह अपने पोते को घोड़े की पीठ पर बिठा वो अब पैदल ही चल देता है।
यह पूरी फिल्म अफगानिस्तान में चल रहे बेमतलब युद्ध से हुए विनाश में मनुष्यता को खोजने की सिनेमाई कोशिश है। अफगानिस्तान पर अमेरिकी बमबारी से क्षतिग्रस्त हुए पुल, मकान, सड़कों, पहाड़ों को सचल लैंड स्केप की तरह फिल्मांकन में प्रयोग किया गया है, जिससे फिल्म के अधिकतर फ्रेम एक उत्कृष्ट कला कृति बन जाते हैं। फिल्म के बूढ़े नायक दस्तगीर की आंखें अतीत के युद्धों का बीता हुआ सब कुछ बिना बोले कह देती है। उसके पोते यासीन की आंखों में देश का भविष्य देखा जा सकता है। एक दादा और पोते की आंखों के रूपक का सिनेमाई दृश्यों में रूपांतरण फिल्म की असली ताकत है।
इस वक्त अफगानिस्तान में जब एक बार फिर से तालिबानी शासन के आसार दिखाई दे रहे हैं, तब कल्पना कीजिए कि जब वो दुनिया से मान्यता लेकर पूरी तरह सत्ता में आ जाएंगे तब वहां की कला, साहित्य, सिनेमा और सेक्युलर संस्कृति का क्या होगा! उनके खत्म हो जाने का संशय बरकरार है, लेकिन हर बार अफगान ही जब जीतें हैं, तब इस दफा दुनिया का ये खूबसूरत कबीलाई देश तालिबान के खिलाफ कैसा प्रतिरोध तैयार करता है, ये देखने वाली बात होगी।

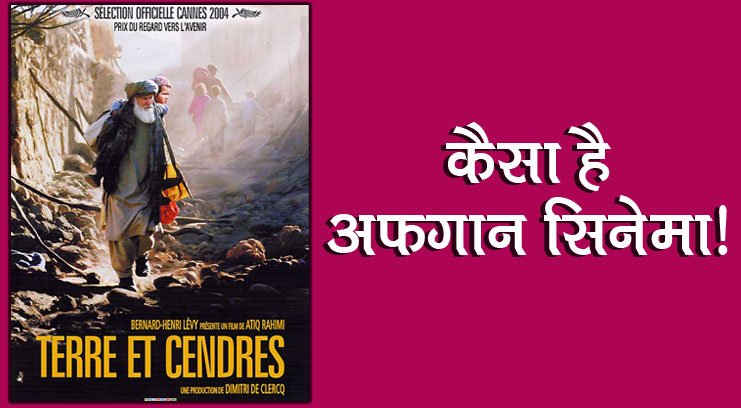


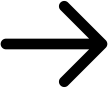
.jpg)







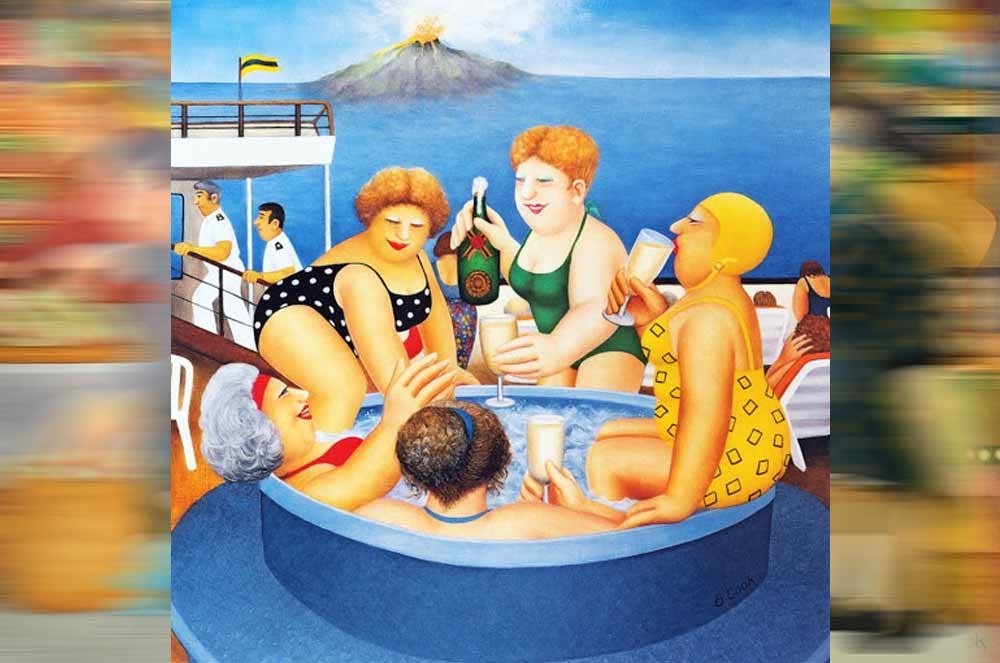











Leave your comment