Newsmanji.com Desk : सत्य के साथ, बिना समझौते के. | 'न्यूजमैन जी' एक स्वतंत्र ई-मैगज़ीन है, जो सत्ता और बाज़ार से परे जाकर जनता के पक्ष की पत्रकारिता करती है. हमारा उद्देश्य है — तथ्य आधारित, गहराई से जांची हुई और दृष्टिकोण से समृद्ध खबरें आपके सामने रखना. हम मानते हैं कि पत्रकारिता केवल “खबरें सुनाने” का काम नहीं, बल्कि “सवाल उठाने” और “सत्ता को जवाबदेह” बनाने का भी दायित्व है.
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तकरीबन गुमनामी की जिंदगी जी रहे एक 80 साल के होने जा रहे हिंदी लेखक को अपने जन्मदिन से ठीक पहले सिर्फ इसलिए व्यापक चर्चा मिल जाए कि उसने खुद पर होने जा रहे शोध के एवज में पैसों की मांग कर ली, तब इसे आप कैसे देखेंगे! ऐसे ही एक दिलचस्प वाकये को लेकर इन दिनों बहस चल पड़ी है। इस बहस का स्वरूप व्यापक हो गया है और इसके साथ ही हिंदी लेखकों को तकलीफ देने वाला 'मानदेय का जिन्न' फिर से वापस लौट आया है।
सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान पर चल रही हवाई बहस, उथली राजनीतिक बहसों, कांग्रेस-बीजेपी के आईटी सेल की बकवास थ्योरी, निजी छींटाकशी और धार्मिक उन्माद को हटा दें तो इस वक्त हिंदी जगत में लेखकों के मानदेय का मुद्दा छाया हुआ है। एक के बाद एक इस मसले पर कई लेखकों ने अपनी बात रखी है। हिंदी में मानदेय को लेकर लेखकों की चिंताएं नई नहीं हैं, बल्कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए समय-समय पर जरूर 'नई वाली हिंदी' जैसे जुमले भी गढ़े गए। आधुनिक वक्त में जब हिंदी लेखकों की दुर्दशा को अब भी 'प्रेमचंद के फटे जूतों' से नापने की रवायत हो, तब इस तरह की बहस नई हलचल तो पैदा कर ही रही हैं।
यह भी पढ़ें: फिर अंधेरे दौर में अफगानिस्तान का सिनेमा!
'मुझे चांद चाहिए' को लेकर पहचाने जाने वाले लेखक सुरेंद्र वर्मा ने असल में एक शोधार्थी से खुद पर शोध के एवज में 25 हजार रुपयों की मांग कर दी। शोधार्थी ने उम्रदराज हो चुके इस लेखक को पैसे तो नहीं दिए, अलबत्ता बातचीत की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग कर उसे वायरल जरूर कर दिया। अब हुआ यह है कि अधिकत्तर हिंदी लेखक सुरेंद्र वर्मा के पक्ष में ही लामबंद हो गए हैं, गोयाकि हिंदी लेखकों की दुखती रग तो एक सी ही है।
हर वक्त 'पैसों के अभूतपूर्व संकट' से जूझते हुए ही 'उम्दा' करार दे दी गई कृतियों को दुनिया के सामने लाने का जोखिम उठाने के बावजूद 'हिंदी का लेखक' बाहुबली नहीं हो सका है। यह दशा साहित्य से लेकर पटकथा लेखन तक बरबरार है। प्रेमचंद के फटे जूते दिखाकर उसे आदर्श स्वरूप देना हिन्दी समाज की धूर्तता है, वैसे ही जैसे यह कहना कि वंचित समुदाय और कृषक वर्ग को सदैव ग़रीब दिखना चाहिए! सुरेन्द्र वर्मा के ऑडियो के वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस मसले को लेकर व्यापक चर्चाएं हो रही हैं।
पूर्व पत्रकार और पटकथा लेखक रामकुमार सिंह ने इस मसले पर तफ्सील से लिखा है। उन्होंने अपनी वॉल पर एक पोस्ट में लिखा- ''मैं पत्रकारिता से बाहर धकेला गया हूं। आज एक पेशेवर लेखक हूं। आज लेखन ही मेरी और मेरे परिवार की आजीविका है। मैं कहीं भी मुफ्त में अपने लेखन कौशल का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं जानता था कि हिंदी साहित्य में लेखन से आजीविका संभव नहीं है। इसलिए मैंने होशोहवास में स्क्रीनराइटर के रूप में खुद को काम करने के लिए मनाया। लेखन या स्क्रीन के लिए लेखन मैंने मेहनत करके सीखा है। काफ़ी समय और धन खर्च हुआ। यह मुझे उपहार में नहीं मिला है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करना सीखता है, जैसे इंजीनियर पुल बनाना सीखता है। वैसे ही कहानी का क्राफ्ट और उसकी दुनिया को सीखने के लिए बहुत कोशिश की है। कितना सीख पाए यह कहना मुश्किल है लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि यह मुफ्त बांटने के लिए नहीं है। नए हिंदी लेखकों के लिए मेरा यह स्पष्ट संदेश है।''
अपनी इसी पोस्ट में उन्होंने लेखकों से पेशेवर होने की उम्मीद जताते हुए लिखा- ''मेरे एग्रीमेंट वित्तीय और कानूनी सलाहकार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें कॉपीराइट एक्ट की सारी धाराओं के बारे स्पष्ट उल्लेख होता है। उसमें भविष्य में बौद्धिक सम्पदा से होने वाली आय की संभावनाओं को वो रेखांकित करते हैं। निर्माताओं से मैं वो जरूरी बदलाव के लिए आग्रह करता हूं। आने वाले समय में कहानी और कंटेंट की दुनिया बहुत विशाल होने वाली है। यह लगभग हो भी गई है। इसलिए आप लेखक हैं तो अपनी कहानियों को मुफ्त में मत बांटिए। आप अपना और आने वाले लेखकों का नुकसान कर रहे हैं।''
यह भी पढ़ें: क्या मोदी ने खुद ही ढहा दिया है अपना 'झूठ का किला'!
'कश्मीरनामा' और 'उसने गांधी को क्यों मारा' जैसी चर्चित किताबों के लेखक अशोक कुमार पांडे ने इस मसले पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है 'मुफ़्त में कुछ नहीं।' इसके अलावा भी उन्होंने इस मसले पर कई पोस्ट लिखी हैं। एक पोस्ट में वो लिखते हैं- ''एक औसत हिन्दी लेखक नौकरी करता है। आठ घंटे की नौकरी। लगातार मानसिक तनाव। घर-परिवार और बाक़ी चीज़ें भी होती हैं। दोस्तियां रिश्तेदारियाँ भी निभानी हैं। इसलिए पढ़ने का वक़्त नहीं मिलता। कई बार पसंदीदा किताब ख़रीदने या कहीं जाकर शोध करने की न फ़ुर्सत होती है न पैसा। फिर जो लिखता है, वह इन सबमें से समय निकालकर। छपना भी शुरुआत में कम समस्या नहीं। दूर दराज़ के लोग कई बार कुछ पैसे देकर ही छप पाते हैं या छप भी गए तो रॉयल्टी की सोच भी नहीं पाते। आपको क्या लगता है इन सबके बाद वह कोई महान रचना लिख पाएगा? अगर लिख पाता है तो वह चमत्कार ही समझिए। सोचकर देखिए अगर लिखने से उसे पैसे मिल जाएं काम भर के और ग़ुलामी न करनी पड़े तो वह कितना बेहतर लिख पाएगा! मुफ़्तख़ोरी ऐसी कि पाठक उससे मुफ़्त में किताब चाहता है, सम्पादक मुफ़्त में लेख, आयोजक मुफ़्त में भागीदारी।''
उन्होंने अपनी इसी पोस्ट में आगे लिखा है- ''हिंदी का पाठक समाज भयावह रूप से असंवेदनशील है लेखक के प्रति। यहाँ लेखन मतलब फ़ालतू काम। यहाँ कोई लेखक को अपने घर बुलाकर एक चाय नहीं पिलाता, उल्टे कहेंगे - हमें खाने पर कब बुला रहे? तो अगर लेखक अपने लिखे के पैसे माँग रहा है, या अपनी मेहनत के बदले पैसे माँग रहा है तो कील ठोंकने तक के पैसे देने वालों को बुरा क्यों लगना चाहिए?''
संजीव चंदन ने इस मसले के बहाने शोध कार्यों पर रोशनी डालते हुए लिखा- ''लेखक-शोधार्थी विवाद: जरा संभल के! जब सुखदेव थोराट जी ने शोध के लिए राजीव गांधी फेलोशिप की शुरुआत की तो उसका सीधा असर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में देखने को मिला। एम ए के बाद गरीब, दलित समाज के विद्यार्थी पीएचडी थोड़ी सुविधा के साथ करते दिखे, ड्राप आउट रुका। उसके बाद और भी फेलोशिप शुरू हुए। सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी। इसके पहले जेआरएफ ही एक मात्र फेलोशिप था, जो यूजीसी देती थी, परीक्षा के माध्यम से। फेलोशिप ने उच्च शिक्षा के माहौल में अभूतपूर्व बदलाव लाये। पीएचडी तक आते-आते विद्यार्थी इस उम्र तक पहुंच जाता है कि उससे घर वालों की उम्मीद जग जाती है, फी देने की जगह छोटे- भाई बहनों में लिए उससे फी की उम्मीद की जाने लगती है। घर की गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। यदि वह फेलोशिप से थोड़ा बहुत घर को योगदान भी कर देता तो फिर मानसिक सुकून के साथ शोध कर सकता था, और यह प्रत्यक्ष रूप से हुआ।
शोधार्थियों का संकट यह है कि एक तो विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शोध का न माहौल है, न प्रेरणा। कुछ को छोड़कर अधिकांश विश्वविद्यालयो में शोध साक्षात्कार के दौरान एक्सपर्ट के खर्चे और ऊपर से पैसे देने के शर्मनाक चलन हैं। जब फेलोशिप मिलने लगा तो देखा कि विवि के शिक्षक , गैर शिक्षक कर्मी इस व्यवस्था से चिढ़ने लगे। विद्यार्थियों की यह सुविधा उन्हें गैरवाजिब लगने लगी। वे खुद भले ही अपने वेतन से शिक्षा में गुणवत्ता की जगह अपने ऐशोआराम में योगदान कर रहे हों। इस पृष्ठभूमि में, खासकर भाषा के विद्यार्थियों/ शोधार्थियों की पृष्ठभूमि के संदर्भ में सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा मांगे गये पैसे के बारे में राय बनानी चाहिए। लेखक पैसे लें तो अच्छी बात है। लेकिन यह परम्परा उन्हें अखबारों, टीवी चैनलों, बड़े पत्रकारों के साथ ज्यादा विकसित करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इस मामले में अधिकांश लेखकों के पोस्ट शोधार्थियों की भर्त्सना वाले हैं या उन्हें मिलने वाले फेलोशिप पर हाहाकार करते हुए। यह भी एक तरह की असंतुलित राय है। लेखकों को पैसे मांगने के लिए लानतें भेजने जैसा ही असंतुलित।''
प्रकाश के रे ने इस मसले पर चुटकी लेते हुए लिखा- ''लिखने और पाने की बहस पर- अगर मूड होता है तो कभी-कभी मैं भी लिख देता हूँ। पैसा मिलता है, तो अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो शिकायत नहीं करता क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि मेरा मन था, लिखा। मैं पूंजी के और रूप को भी महत्व देता हूं- कल्चरल/सोशल कैपिटल। और, फिर यह भी कुछ लोगों तक बात तो पहुंची, सोचकर संतोष होता है। वैसे भी पैसे का करना क्या है, मुझ आत्मसंतोषी संत स्वभाव मितव्ययी व्यक्ति को। माया से दूर रहना चाहिए।''
सुयश सुप्रभ ने अपनी वॉल पर इस मसले को लेकर कुछ पोस्ट की हैं। इनमें से एक में वो लिखते हैं- ''लेखक को इंटरव्यू के लिए पैसा मिलना चाहिए। सही बात है। सुरेंद्र वर्मा ने पैसा मांगा तो उन्हें विश्वविद्यालय के स्तर पर पैसा देने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। शायद लोग भूल गए हैं कि इस देश में शोधार्थी को महीनों स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती। अब बात करते हैं पीएचडी की। लोग ऐसे विषयों पर पीएचडी कर रहे हैं जो न समाज की बेहतरी से जुड़े होते हैं और न ही भाषा-साहित्य की बेहतरी से। क्या यह सिर्फ़ शोधार्थियों की नासमझी का नतीजा है? नहीं। भ्रष्टाचार की तरह ऐसी नासमझियों की गंगा भी ऊपर से नीचे बहती है। मतलब ज़िम्मेदारी हिंदी विभागों की भी बनती है। किसी लोकप्रिय लेकिन दिशाहीन लेखक के लेखन पर सालों मेहनत करके क्या हासिल होगा? विदेशी विश्वविद्यालय शब्दकोशों से लेकर साहित्यिक पत्रिकाओं तक गुणवत्ता के पैमाने पर कई शानदार मिसालें सामने रख चुके हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों से ऐसी उम्मीद क्यों नहीं की जानी चाहिए? हमारे यहां सूरदास और तुलसीदास की काव्यदृष्टि से बात आगे बढ़ने में दशकों लग गए। लेकिन क्या ऐसे शोधार्थी सामने आ रहे हैं जो हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने की दिशा में कुछ ढंंग का काम करते नज़र आ रहे हों?'' हालांकि, ठीक इससे पहले की एक पोस्ट में वो सुरेन्द्र वर्मा पर ही तंज कसते हुए लिखते हैं- "सुरेंद्र वर्मा पर पीएचडी कैसे हो रही है, बहस तो इस पर भी होनी चाहिए थी। हिंदी विभागों ने सचमुच हिंदी की बहुत दुर्दशा की है।"
रंगनाथ सिंह ने अपनी वॉल पर लिखा है- 'हिन्दी साहित्य और पैसे का छत्तीस का आँकड़ा है। पैसे का जिक्र आते ही हिन्दी साहित्य की शान्ति में खलल पड़ जाता है। यहाँ गरीबी जीवन-मूल्य की तरह स्थापित है। लोग भूल जाते हैं कि समूचा बौद्धिक कर्म एक मध्यमवर्गीय उद्यम है। तोल्सतोय या रवींद्रनाथ ठाकुर की तरह पैसे-रुपये से बेफिक्र होकर लिखने का सौभाग्य तभी मिलता है जब आपके पास पुश्तैनी जमीन-जायदाद हो। दूसरी सुखद स्थिति है कि आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हों और बचे हुए समय में रुपये-पैसे से बेफिक्र होकर नेम और फेम के लिए अतिरिक्त उद्यम कर रहे हों। 80 वर्षीय सुरेंद्र वर्मा जी के जीवन की मूल चिन्ता है, पैसा। जिस पैसे से उनकी दवा-दारू आती होगी। दाना-पानी चलता होगा। फोन-पानी का बिल भरते होंगे। अन्य जरूरी जिम्मेदारियाँ होंगी। आज के जमाने में 'पैसा हाथ का मैल है', वही कहेगा जिसके हाथ में पैसा कमाते समय मैल नहीं लगता। कुछ लोग लेखक को एक साधारण व्यक्ति की तरह देखने के बजाय ईसा मसीह की तरह देखने के आदी हो चुके हैं।'
यह भी पढ़ें: सुपिन मेरे ख्यालों की नदी है, जिसके ऊपर लायबर दौड़ रहा है!
बहरहाल, इससे पहले मार्च में नई वाली हिंदी के पोस्टर ब्वॉय दिव्य प्रकाश दुबे भी सोशल मीडिया पर 'नो टु फ्री' कैंपेन चला चुके हैं। उन्होंने तब लेखकों से अपनी भागीदारी और काम के एवज में पैसे मांगने का पक्ष मजबूती से रखा था। उनके मुताबिक लेखकों को अपने काम के एवज में पैसे मांगने से हिचकना नहीं चाहिए। बहरहाल, सुरेन्द्र वर्मा के बहाने ही सही, एक बार फिर से हिंदी जगत में लेखकों के मेहनताने को लेकर नई बहस तो छिड़ी हुई ही है। इस बहस से वास्तविक धरातल पर क्या बदलाव आ सकेंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो सुरेन्द्र वर्मा के साल 2010 में ‘भारतीय ज्ञानपीठ’ से प्रकाशित उपन्यास ‘काटना शमी का वृक्ष पद्मपखुंरी की धार से’ के उस उद्धरण का ख्याल आता है, जहां वो लिखते हैं- 'जिनके पास साधन होते हैं, उनके पास दृष्टि नहीं होती, जिनके पास दृष्टि होती है- केवल वही होती है, और शून्य होता है...' या फिर 'परित्याग करो और सुखी हो जाओ।'

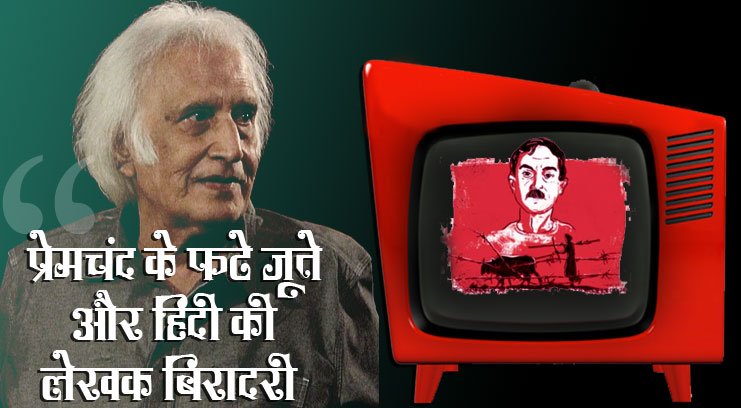

.jpg)







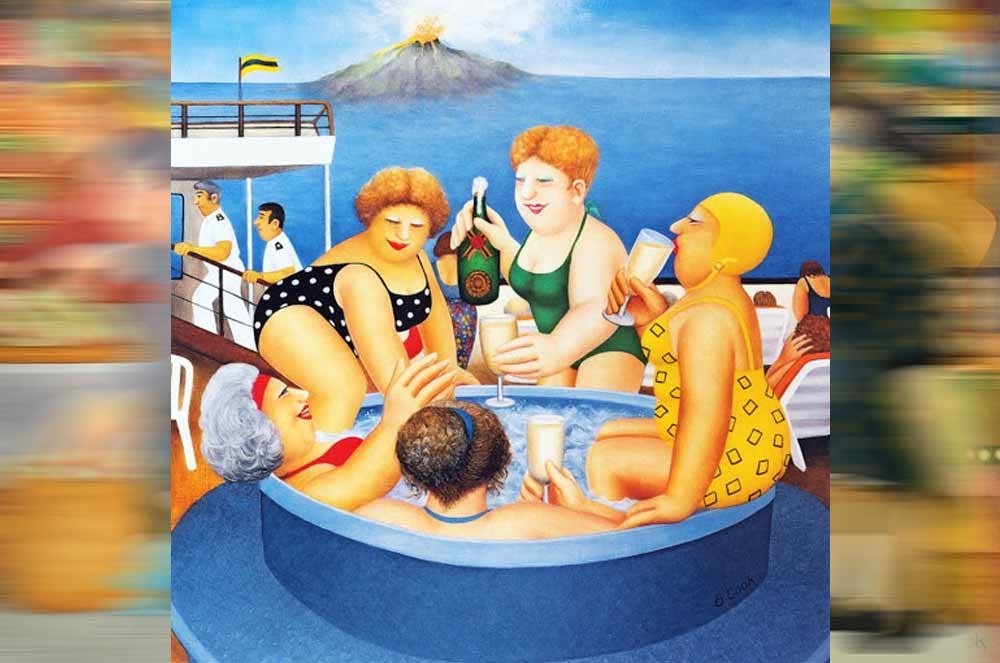

.%5B1%5D.jpg)









Leave your comment