केशव भट्ट उत्तराखंड के एक हिमालयी कस्बे बागेश्वर में रहते हैं। केशव को ढूंढना बेहद आसान है। बागेश्वर में उनकी एक मिठाई की दुकान है, लेकिन यही उनकी पहचानभर नहीं है! असल में केशव ने लंबे वक्त तक अखबारों के लिए लेखन किया है और इससे भी बढ़कर उन्होंने हिमालय के अलग-अलग हिस्सों को नापा है। केशव का लेखन ताजगी से भरा हुआ है और इससे गुजरते हुए वो आपको अपने साथ हिमालय के दर्रों और घाटियों में चुपचाप लिए चलते हैं। 'हिलांश' पर केशव के किस्सों की एक पूरी खेप आ रही है।
रुक-रुक कर मुनस्यारी में उस रोज देर रात तक बारिश होती रही। आंख खुली तो भुरभुरी ठंड महसूस होने लगी थी। पहाड़ नहाधोकर चमक उठे थे। सुबह जल्दी ही हम लोग मुनस्यारी से अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। इस रास्ते पर मैं लंबे वक्त बाद लौट रहा था। काफी कुछ वैसा ही था, जैसे पिछली दफा देखा था, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया था। हिमालय के टूटने और बनने के निशान ने भूगोल को थोड़ा सा बदल दिया था। लगभग बारह साल पहले गोरी नदी के उफान ने पंचपाल उड्यार (गुफा) से रड़गाड़ी के लिए नीचे की ओर जाने वाला रास्ता तोड़ दिया था, तब से ऊपर पहाड़ी से एक किमी का अतिरिक्त फेर लगाकर यहां पर आगे जाना होता है।
रड़गाड़ी बेहद दिलचस्प जगह है। यहां पहले शामाधूरा (बागेश्वर) से आए हुए कोरंगा ने निगाल की हट बनाकर यात्रियों के ठहरने के लिए पड़ाव बनाया था, लेकिन आज यहां सब बदला-बदला सा दिख रहा था। लकड़ी के पुल की जगह लोहे के पुल ने ले ली थी। निगाहें कोरंगा को ढूंढ रही थी। चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोरंगा की हट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था।
पुराने रास्तों पर लौटने में आप पुराने लोगों को ढूंढने लगते हैं। मैंने भी वही किया और आस-पास के लोगों से कोरंगा के बारे में पूछने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कोरंगा अब इस दुनिया में नहीं था। एक रोज गोरी नदी उसे अपने साथ वीरान पहाड़ों से उठाकर ले गई। असल में मुझे पता चला कि गोश्त का शौकीन रहा कोंरगा गोरी नदी के पार मुर्गी के शिकार की तीव्र इच्छा को दबा नहीं पाया और उसने उफनती गोरी नदी के उस पार जाने के लिए लकड़ी के लट्ठ डालकर पुल बनाने की कोशिश की। वो कामयाब भी हो जाता, लेकिन अचानक वो लकड़ी से अपनी पकड़ खो बैठा और फिसल कर गोरी के तेज बहाव में गायब हो गया। कोरंगा को बस लोगों ने कुछ सेकेंड के लिए पानी से बाहर निकलते हुए देखा और फिर वो हमेशा के लिए पहाड़ों से गायब हो गया। पहाड़ों के अपने जोखिम है, जिन्हें भोगना आसान नहीं।
अब यहां ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन थोड़ा ही आगे स्यूनी में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के रुकने की व्यवस्था कर रखी है। हम गोरी के ठीक ऊपर से गुजर रहे थे और नीचे गोरी बौखलाए सांप सी फुंफकार कर बह रही थी। गोरी की चपेट में आयी चट्टानों के पत्थर कई तरह की मूर्त-अमूर्त आकृतियों का समूह का सा आभास करा रहे थे। साल दर साल पानी की चोट ने चट्टानों को कलाकृतियों में बदल दिया था, जिसे देखने के लिए नजर चाहिए।
हम स्यूनी पहुंच गए थे। यहां हमने देव सिंह सुमटियाल की झोपड़ी में हल्का नाश्ता किया ओर आगे बढ़ गए। पंचपाल उड्यार से स्यूनी लगभग चार किमी दूर है और यह रुकने के लिए एक सुंदर पड़ाव है। बोगडयार पहुंचते-पहुंचते सूरज हमारे सिरी के ऊपर आ गया था। यहां हमने दिन का खाना खाया और थोड़ी देर सुस्ता कर आगे बढ़ गए। बोगडयार तकरीबन 2600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है।
मिलम की ओर बढ़ते हुए हमने रास्ते में ‘नहर पानी’ में एक बार रूकने का इरादा बना लिया था, लेकिन फिर इसे हमें जल्दी ही बदलना पड़ा। हमने तय किया कि हम आगे ‘लास्पा गाढ़’ तक पहुंचेंगे और रात को वहीं डेरा डालेंगे। लास्पा गाढ़ पहुंचते-पहुंचते घुप्प अंधेरा हो गया था। बारिश से रास्तों पर फिसलन हो गई थी। लास्पा गाड़ी में फिसलन भरी चढ़ाई को पार कर हम आखिरकार कौशल्या आमा की ढलान में बनी हुई उस झोपड़ी में पहुंचे, जहां हमें रात गुजारनी थी। हमारे बाद कुछ नेपाली मजदूरों का झुंड भी वहां आ गया, लेकिन आमा ने उन्हें ‘मेहमान आएं हैं’ कहकर अपनी मजबूरी जता दी।
नेपालियों का वो झुंड आगे स्यूनी पड़ाव की ओर चल पड़ा। उनके निकलते ही आमा ने हमें बताया- ‘ये आईटीबीपी का सामान ढोते हैं। इन्हें आदत है दिन-रात चलने की। अक्सर ये मजदूर तो मिलम से एक ही दिन में मुनस्यारी पहुंच जाते हैं।’ रात को आमा ने हमे इलाके की कई गतिविधियों से वाकिफ करवा दिया था।
हम अपने मैट्रेस निकाल अपनी जगहें बनाने में जुट गए। कुटिया छोटी व लंबी थी, जिसके दो हिस्से थे। एक में मुसाफिर ठहरते थे और दूसरे में दोनों बूढ़े। आमा और उनके पति। चूल्हे में जलती लकड़ियों की आग से कुटिया अच्छी खासी गर्म हो गई थी। लास्पा गाढ़ का 'सुसाट-गुर्राट' (शोर) आमा की बातों में दब गया।

आमा भोजन की जुगुत में जुटी हुई थी। चूल्हें में जिस वक्त वो आग सुलगाने में मशगूल थी, मैंने उनसे पूछ लिया- ‘यहां से लास्पा गांव कितनी दूर है?’ आमा ने बिना मेरी ओर देखे ही चूल्हे में फूंक मारते हुए जवाब दिया- ‘दो किमी ही होगा, वहां पहुंचने में हमें आधा-एक घंटा लगता है।’ आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक के दरमियान आमा ने कई सारी बातें हमें बताई। आमा ने कहा- ‘गांव में 30 के आसपास मवासे (परिवार) हैं। दसवीं तक जनजाति स्कूल के साथ ही गांव में प्राइमरी स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ने के नाम पर 15-16 बच्चे होंगे। वो भी स्कूल नहीं जाते हैं। घर वाले ही नहीं भेजने वाले हुवे। अब ऐसे में मास्टर भी क्या करेगा! मास्टर लवराज लसपाल तो पढ़ाने वाला हुवा ही, लेकिन कोई पढ़ने वाला तो हो।' आमा ने एक झटके में इलाके में शिक्षा को लेकर स्थिति साफ कर दी थी।
इसके बाद आमा अपने पनरिवार के बारे में बताने लगीं और कहा- 'बेटा हमारा परिवार भी छोटा ही है। दो लड़के हैं। लड़की का धारचूला में ससुराल है। बड़ा लड़का, बहू व नाती ऊपर लास्पा गांव में ही हैं। गांव में बन रहे चैक डैमों में लड़का मजदूरी कर रहा है।' फिर अचानक छोटे लड़के का उत्साह से जिक्र कर, यह कहते हुए उदास हो गई- छोटा लड़का प्रकाश गाने के साथ ही ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी में माहिर है। धरती को देख कर उसके बोल फूट जाते हैं। बेटा... ऐसे-ऐसे गाने गाता है कि हर कोई मगन हो जाता है। गांव की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ने के लिए मुनस्यारी में जाने को तैयार ही नहीं है। वहां जनजाति स्कूल में सब सुविधाएं हैं। हम गरीब लोगों के लिए ये जनजाति वाले स्कूल ही हुवे। अब ये बात प्रकाश को कैसे समझाएं!’
इतनी देर में खाना भी तैयार हो गया था। भात, दाल, रोटी व जोहार के खेतों के पालक की टपकी। आमा ने अपने मेहमानों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बेहद प्यार से उस शाम आमा ने हमें खाना खिलाया और फिर अगली सुबह की तैयारियों को पूरा कर सो गई। खाना खा चुकने के बाद नींद में लास्पा गाढ़ का शोर अब लोरी की तरह लग रहा था।
सुबह नींद जल्दी खुल गई थी। हम अपने तय समय से एक पड़ाव पीछे चल रहे थे। हमने तय किया कि आज हम मिलम तक पहुंचेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। हम सभी धीरे-धीरे ऊंचाई के साथ सामंजस्य बिठा रहे थे। आमा-बूबू से विदा लेकर हम तिरछे व उतार-चढ़ाव वाले रास्ते पर बढ़ गए। गोरी यहां शांत बह रही थी। रिलकोट से पहले नाहर देवी का मंदिर भी है। रिलकोट पहुंचने में ही दो घंटे लग गए। रिलकोट की ऊंचाई 3200 मीटर है। यहां मौजूद इकलौती दुकान में दाल-भात बन रहा था, जिसने हमारे कदमों को रोक दिया। हमने तय किया कि आज मिलम के बजाए मार्ताेली में ही रूका जाएगा। असल में हम रिलकोट में ही बन रहे दाल-भात को निपटाने के मूड में थे और इससे देरी होना तय था।

(रिलकोट में...)
रिलकोट गांव खाली-खाली सा दिखा। पांच मकान पत्थर की छत वाले और एक में टिन डली हुई थी। बगल में ही एक सरकारी बिल्डिंग बन रही थी। गांव के नीचे बह रही गोरी नदी के किनारे बकरियों के झुंड फैले हुए थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे सामने दाल-भात की थारी परोसी जा चुकी थी। खाने के सुख के बाद जब हम मुख्य रिलकोट गांव की धार (चोटी) में पहुंचे तो वहां हमें कुछ खंडहर मिले। हम सोच रहे थे कि चारों ओर से खुली व असुरक्षित इस धार में ना जाने क्यों ये गांव बसाया गया होगा। तीखी हवाओं व बर्फ के तूफानों को ये गांव ज्यादा वर्षों तक शायद झेल नहीं सका और फिर लोग नीचे आकर बस गए। ये गांव उनके जाने के बाद से ही शायद उजाड़ हो गया हो।
यहीं से दूर सुंतो गाढ़ (नदी) के किनारे सुंतो गांव के खंडहरों के अवशेष भी दिखाई दे रहे थे। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में सुमटियाल, टोला व टोलिया गांव में कुछ बुढ़े-बुजुर्गों के कपड़े आंगन में सूख रहे थे, जो उनके होने का अहसास करा रहे थे। ये सारे गांव ना जाने क्यों मुझे सहमे-सहमे से लगे। इन गांवों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।
कुछ दूर चलने पर एक जगह दो रास्ते नजर आए, जिसके छोर पर गांव के नौजवानों ने एक बोर्ड लगाया था, जिसपर लिखा था- ‘मार्ताेली में आपका स्वागत है।’ यहां पर ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता मार्ताेली गांव को और नीचे की ओर जाता रास्ता आगे चलकर बूर्फू की ओर जाने वाले रास्ते में मिलता है। हम लगातार बुग्याली घास पर चल रहे थे, जिससे हमारी थकान जाती रही। भेड़ों का झुंड बुग्यालों से वापस नीचे की ओर उतर रहा था। मार्ताेली की सीमा में पहुंचते ही दूर से ही एक मकान की दीवार में सफेद चूने से बड़े से अक्षरों में ‘राजू होटल’ लिखा दिखा, तो उसी ओर कदम बढ़ चले। उसके आंगन में पहुंचे तो एक नौजवान नजर आया। हमने उसे डॉ मर्ताेलिया का परिचय दिया, तो वो अतिरिक्त आत्मीयता से भर उठा। उसका नाम राजू था। राजू ने दो मंजिले की चाख में एक ओर हमारे रुकने की व्यवस्था कर दी थी। दूसरे हिस्से में कुछ घोड़े वाले रुके हुए थे। रात अच्छी कटी।
इस गांव के शीर्ष में मां नंदा का भव्य मंदिर है। नंदा देवी को हिमालय की बेटी कहा जाता है और उसकी कई लोककथाएं हैं। हिमालय का कुंभ असल में 'नंदा के ससुराल' यानी कि कैलाश जाने की यात्रा का आयोजन होता है। हर बारह साल में यहां लोग उमड़ते हैं। अगली सुबह मौसम साफ देख हम नंदा देवी मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर गांव से करीब किलोमीटर भर दूर होगा। लगभग 3440 मीटर की ऊंचाई पर बसे मार्ताेली में अभी चार मवासे ही खेती-बाड़ी के लिए लौटे थे। मंदिर के रास्ते में कुछ खेत उपजाऊ थे।
अचानक हमारी नजर किनारे पर खंदक पर पड़ी तो कौतुहल वश उधर लपक पड़े। इन्हें खंदक कहें या टैंच! ये असल में फौज ने बनाई थी। ये खंदकें 1962 में चीन के आक्रमण की कहानी बयां कर रही थी। नीचे दूर ल्वां गाड़ का शोर यहां तक सुनाई दे रहा था। ल्वां गांव इस छोर का अंतिम गांव है। ल्वां में मात्र दो परिवार ही अपनी गुजर-बसर के लिए अब मजबूरी में रहते हैं। ल्वां गांव से ही नंदा देवी ईस्ट पर्वत के साथ ही लॉन्ग स्टफ कॉल, नंदा कोट सहित कई हिम श्रृखंलाओं को फतह करने के लिए पर्वतारोही दल जाते हैं।
18 वीं सदी में जब सड़के नहीं थी, तब व्यापार के लिए पिंडारी ग्लेशियर के शीर्ष में ट्रेल दर्रे को पार करने के बाद ल्वां ग्लेशियर होते हुए ल्वां गांव पहुंचना होता था। ग्लेशियर की वजह से यह मार्ग काफी खतरनाक होता चला गया, तो इस दर्रे से आवाजाही बंद ही हो गई। हांलाकि 19 वीं सदी में अंग्रेज शासक जार्ज सर ट्रेल ने इस दर्रे से एक बार फिर से आवाजाही शुरू करने के ख्याल से इसे पार करने की सोची, लेकिन वो अपने अभियान में सफल नहीं हो सका। हालांकि, उसके साथ गया सूपी गांव का मलख सिंह यह दर्रा पार करने में सफल रहा। बाद में इस दर्रे को ट्रेल दर्रे का नाम दे दिया गया।

हल्की चढ़ाई के बाद ही हमें गांव के शीर्ष पर बने हुए नंदा देवी के मंदिर के दर्शन हुए। मंदिर के चौक में पत्थरों के बने हुए चूल्हे अब भी दिख रहे थे। पिछले दिनों नंदा पूजा में यहां काफी परिवार पूजा के लिए आए आए होंगे ओर ये चूल्हे उन्हीं ने लगाए होंगे। नंदा देवी के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा के चलते प्रवासी साल भर में एक दफा नंदाष्टमी के दिन यहां खिंचे चले आते हैं। घाटियों के लोग अपनी देवी के पास लौटते हैं और समृद्धि की खोज में फिर से मैदानों की ओर लौट जाते हैं। ये लोगों के सामाजिक मिलन का वक्त भी होता है।
इस दौरान करीब महीने भर के लिए जोहार घाटी नंदा देवी के जयकारों से गूंजती रहती है। गांव में सामूहिक भेज के आयोजन हों या फिर बैठकियों का दौर, ये वक्त गुलजार और खुशनुमा होता है। उस दौरान मंदिरों में पूजा-अर्चना के साथ ही गांवों से आनी वाली टोलियों का मिलन देखने लायक होता है। हिमालय की बसावटों को करीब से देखने का अपना सुख है। मैंने मंदिर की चौखट पर नजर मारी तो वहां कुछ लिखा हुआ था-
‘‘छिला ताछी तुछी कुटालीक, हाली छ बीन।
छिला नंदा देवी सेवा कौल, बरसी दीन।
छीला बाटा तली सर्प छड़ी, बाटा मली सर्प।
छिला नंदा देवी दैन हये, सबों की तरफ।’’
मौसम को करवट बदलते देख नंदा देवी के मंदिर से हम वापस लौटने लगे। पहाड़ों पर मौसम घिरने के बाद यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बारिश कितनी देर चलेगी। हम तेजी से गांव में लौट आए थे। हम मार्ताेली गांव की गलियों में भटक रहे थे। जिन गलियों में कभी बच्चे चहकते होंगे, वो गलियां अब सुनसान सोई हुई सी महसूस हो रही थी। एक अजब सी उदासी पसरी हुई थी, मानों गांव उजड़ गया हो। 200 मवासों (परिवारों) का गांव आज सुनसान था। ज्यादातर मकानों की छतें और दीवारें टूट चुकी थीं। उनके टूटे दरवाजों पर लटके हुए ताले, उनके मालिकों के अब न लौटने की कहानी बयां कर रहे थे। ये हाल पहाड़ के कई हिस्सों का अब हो चला है... गांव के गांव खाली हैं।




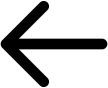 Previous
Previous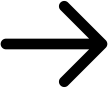





















.%5B1%5D.jpg)









Leave your comment