केशव भट्ट उत्तराखंड के एक हिमालयी कस्बे बागेश्वर में रहते हैं। केशव को ढूंढना बेहद आसान है। बागेश्वर में उनकी एक मिठाई की दुकान है, लेकिन यही उनकी पहचानभर नहीं है! असल में केशव ने लंबे वक्त तक अखबारों के लिए लेखन किया है और इससे भी बढ़कर उन्होंने हिमालय के अलग-अलग हिस्सों को नापा है। केशव का लेखन ताजगी से भरा हुआ है और इससे गुजरते हुए वो आपको अपने साथ हिमालय के दर्रों और घाटियों में चुपचाप लिए चलते हैं। 'हिलांश' पर केशव के किस्सों की एक पूरी खेप आ रही है।
(भाग - 4) मौसम को करवट बदलते देख हम सही वक्त पर नंदा देवी के मंदिर से अपने रात के ठिकाने पर वापस लौट आए थे। 'शाम के खाने में दाल-चावल या फिर कुछ और?’ राजू ने पूछा तो तन्द्रा टूटी। कुछ और में क्या है...? होता क्या है यहां...! सूखा मीट है। वही बना दूं क्या।' संजू ने आंखे तरेरी, मानो राजू ने कुछ गलत पूछ लिया हो। अब भला शाकाहारी शख्स को गोष्त के स्वाद से क्या मतलब! उसके लिए हरी सब्जी के साथ चावल का विकल्प मिल गया था। सूखा मीट खुद बनाने की जिद हमारे लिए महंगी साबित हुई। मीट का जायका हमारे स्वाद के अनुसार नहीं रहा। उसका स्वाद इतना खराब था कि हममें से सभी ने उसे थोड़ा ही खाया और फिर दोबारा सूखा गोश्त कभी नहीं खाने की कसम खाकर, हमने अपने पेट भरने का अहसास कर लिया। जब तक गोश्त नहीं तैयार हुआ था, तब तक उसकी शान में हमने कसीदे पढ़े, लेकिन मुंह से एक कौर छुआते ही कहानी बदल गई।
उच्च हिमालयी बसावटों में सूखे गोश्त को खाने का चलन है। जोहार, व्यास, दारमा और गढ़वाल हिमालय से सटे ऊंचाई वाले ईलाकों में भेड-बकरियों के मांस को सुखा कर, माला बनाकर संभाल दिया जाता है। इसका उपयोग जरूरत के वक्त होता है और वो जरूरतें पैदा होती हैं, सर्दियों के दरमियान। सदियों पहले इन घाटियों में रचे-बसे लोग बारहमास यहीं रहते थे, फिर चाहे दस फीट बर्फ गिरे या दो... उन्होंने खुद को पहाड़ों पर ढाल लिया था। जीवन की चुनौतियों पर उन्होंने काबू पाना सीख लिया था और तब हिमालय के हिस्से गुलजार रहा करते थे। आज की तरह तब जाड़ों में यहां के बाशिंदे निचले इलाकों में पलायन नहीं करते थे। जाड़ा हो या बर्फबारी हर हालातों से बचाव के लिए उन्होंने अपने तरीके विकसित कर लिए थे।

लगभग छह माह, अप्रैल से सितंबर मध्य तक के खुशगवार मौसम में यहां जिंदगी काफी तेजी से दौड़ती थी। खेती-बाड़ी, जानवरों के चारे की व्यवस्था के साथ ही तिब्बत की मंडी में व्यापार के लिए भाग-दौड़ में ही छह माह गुजर जाते। इसी दौरान गर्मियों में वक्त निकाल कर परिवार के परिवार भेड़-बकरियों के मांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में सुखा कर माला बनाते चलते हैं। यही सूखा मांस बर्फीले दिनों में काम आता है।
अक्टूबर से मार्च तक ये घाटियां बर्फ से लकदक हो जाती हैं। रास्ते कई फीट बर्फ में दबे होते हैं और घरों की छतों से दिनभर पिघलती बर्फ को देखा जा सकता है। सर्दियों के दिनों में ये बसावट एक नजर में हिमालय का आभास करा देती हैं, जहां बर्फ के सिवाय और कुछ नहीं होता। ये छह महीने जोहार वासियों के लिए काफी कष्टकारी होते हैं। गर्मियों में छह माह तक की गई मेहनत के बलबूते ही उच्च हिमालयी इलाके के ये लोग सर्दियों के छह महीने काटते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में रहने वाले लोगों में इन्हें मानिए।
अगले दिन हम मिलम गांव के लिए सुबह-सुबह ही निकल पड़े। मार्ताेली से नीचे नई बन रही सड़क तक हमें तीखा ढलान मिला। इस ढलान पर उतरना मुश्किल था। सामने के पहाड़ पर बसा बुर्फू गांव भी वीरान और खंडहर सा दिख रहा था। सड़क के किनारे बनी झोपड़ी नुमा दुकान के बाहर एक परिवार मीट की माला बनाकर उसे सुखाने में व्यस्त था। गोरी नदी की फुंफकार की वजह से उन्हें गप्पे मारने के लिए आपस में जोर-जोर से बोलना पड़ रहा था। उन्हें देखकर हमें रात के सूखे मीट की याद हो आई और हम मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। बुर्फू के नीचे सड़क के लिए बुग्याल काटे जा रहे थे।

सड़क काटने की वजह से इन बुग्यालों का सौन्दर्य अटपटा सा लग रहा था। दूर सामने मापा गांव भी सुनसान नजर आ रहा था। इन गांवों को देखकर लग रहा था कि भला कैसे लोग साल दर साल इन्हीं जगहों पर काट देते होंगे! उनके पास मनोरंजन के क्या साधन होते होंगे...? वो अपनी जिंदगी में बाकी दुनिया का हाल तब कैसे जानते होंगे!हम इन्हीं बातों के बीच बिल्जू गांव पहुंच गए थे। बिल्जू के उस पार गनघर गांव ऊंचाई पर दिख रहा था। पांचू गांव के बगल में ही पांचू नदी बहते हुए नीचे गोरी से मिलने के लिए दौड़ लगा रही थी। ये एक सुंदर गांव हैं। बिल्जू गांव में हमें घनष्याम मिला, जिसके घर पर हमने दिन का भोजन किया। घनष्याम बिल्जवाल ने बातचीत में बताया कि वो लोग सितंबर के अंत में दुम्मर या फिर मुनस्यारी जैसे निचले इलाकों में चले जाते हैं।
गांव के लगभग सभी लोगों के बसेरे अब निचले इलाकों में भी हैं। कई लोग सरकारी सेवाओं में भी पिछले कुछ दशकों में पहुंचे हैं। सर्दियों गुजरने के बाद उच्च हिमालयी इलाकों के ये गांव वापस गुलजार होने लगते हैं। अप्रैल में गांव के गांव निचले इलाकों से वापस अपने मूल गांवों की ओर लौअ आते हैं। जाने और लौटने की ये पूरी प्रक्रिया जितनी दिलचस्प है, ये उतनी ही मुश्किल भी होती है। अप्रैल के महीने में जब निचले इलाकों से गांववाले वापस अपने घरों में पहुचते हैं, उस वक्त अक्सर गांव बर्फ से ढके हुए मिलते हैं।
घनष्याम ने हमें बताया कि उसकी गुजर-बसर किसी तरह से चल भर रही है। गांव के लिए उस वक्त सड़क बन रही थी। घनष्याम ने कहा- 'ये पूरी कब तक बनेगी, मालूम नहीं। क्या पता सड़क आने से कुछ ठीक हो जाए। शायद तब मैं यहां एक दुकान चला लूंगा।' पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जितनी तेजी से सड़कों का जाल फैला है, उसने पर्यावरण को जरूर बेतहाषा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक सच यह भी है कि लोगों को कई-कई दिन पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के कष्टों से मुक्ति भी मिली है। सुदूर पहाड़ों पर जाती सड़कें उम्मीदें लेकर भी पहुंची हैं।

मिलम से पहले तिब्बत से आने वाली कोलिंगाणा नदी
मिलम ग्लेशियर नौ ग्लेशियरों से मिलकर बना है। ये करीब आधा किलोमीटर चौड़ा और 18 किमी लंबा है। हरदयोल शिखर के वक्षस्थल पर मिलम ग्लेशियर मौजूद है। भोजन के बाद कुछ देर हमने आराम किया और फिर मिलम गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और हमारे कंधों पर वजन था। कहीं रास्ता तीखी खड़ी छलान लिए हुए मिलता तो कहीं खड़ी चढ़ाई। इस दौरान न जाने कितने नाले और झरने पार हो गए। न जाने कितने पत्थरों को हमने लांघ दिया था। ये यात्रा अपनी जमीन के भीतर के हिस्सों को करीब से देखने की यात्रा भी थी और हिमालय के भीतर विचरने का सुख भी।
हम सड़क पर चल रहे थे। इसने बुग्याली रास्ते में पैदल चलने का एहसास छीन लिया था। नीचे खाई में दूर एक टूटी हुई जेसीबी मशीन दिख रही थी। सड़क के लिए बुग्यालों को काट रही इस जेसीबी पर प्रकृति ने अपना गुस्सा उतारा था। धीरे-धीरे दिन तेजी से ढल रहा था। हम कहीं हांफते, कहीं ठहरते, कहीं सुस्ताते तो कहीं अपने कदमों को गति देते। मिलम पहुंचते-पहुचते हमें रात हो गई थी।
मिलम पहुंचकर हम आईटीबीपी के कैंप में पहुंचे। आईटीबीपी को पहुंचने की सूचना देना जरूरी है। आईटीबीपी को जब हमारे मलारी अभियान का पता लगा, तो वो आनाकानी करने लगे। उनका व्यवहार देख एक पल के लिए लगा कि हम किसी तहसील में कोई प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए हों, जहां का कोई घाघ बाबू हमें टरकाने के लिए कई तरह के जतन कर रहा हो! आईटीबीपी के अफसरों ने हमें मिलम से आगे जाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। हम इतनी दूर चलकर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। हम अड़ गए। हम उनकी बेरुखी और अक्खड़पन देखकर भीतर से परेशान भी हो रहे थे। वो हमारा वक्त जाया कर रहे थे, जिसके कोई मायने नहीं। हम अपनी ही जमीन पर रोक दिए गए थे।

हमने अपना आखिरी दांव चला और हौसला बटोरकर थोड़ा डटकर कहा- ‘इस परमिट में परमिशन ना दिए जाने का कारण लिख दो!’ ये सुनते ही वहां मौजूद इंस्पेक्टर उचक गया और उसने लगभग ऐलानिया लहजे में कहा- 'ऊपर काफी बर्फ आ गई है। अभी लॉंग रूट पेट्रोलिंग पार्टी लौटी है। बड़ी मुश्किल से वो लोग यहां पहुंचे हैं। तुम सब बर्फ में फंस जाओगे, तो हम सभी के लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब तुमने जाना ही है, तो एक बार फिर सोच कर देख लो। नहीं तो एक-आध दिन यहीं रहो और वापस लौट जाओ।'
इसके बाद हमारी जामा-तलाशी ली गई। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद हम गांव की फिजा की ओर दौड़ पड़े। हमारे गाइड मनोज ने गांव में एक परिवार के घर पर हमारे रुकने का इंतजाम कर दिया था। अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। जिस घर में हम ठहरे हुए थे, उस घर में रहने वाले परिवार के सदस्य काफी खुशमिजाज किस्म के लोग थे। चाय पीकर हम अब गांव में तफरीह के लिए निकल गए थे। दूरस्थ इलाके के गांवों में अब भी अपनापन जिंदा है।
(भाग- 1) अंटार्कटिका में लॉकडाउन और 224 घंटों की वीरान डरावनी जिंदगी
मिलम गांव तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। एक जमाने में इस गांव में 500 मकान थे, लेकिन अब ये गांव खंडहर हो चुका है। बीते वक्त में गांव की गलियां भूलभूलैय्या सी थीं। इस गांव के बारे में कहावत थी कि, गांव में नई दुल्हन के साथ परिवार का एक सदस्य कुछ माह तक रास्ता दिखाने के लिए रहता था। वक्त के बीतते-बीतते अब खिड़की-दरवाजों की बेहतरीन नक्काशी भी गायब होने लगी है। दरवाजों के साथ ही छत की बल्लियां भी ना जाने कहां लुप्त हो गई हैं। आलू के अलावा अब खेतों में जड़ी-बूटी भी उग रही है।
मिलम में गोरी नदी के किनारे किलोमीटर भर वाला लंबा मैदान है। कभी इसमें गांव वाले खेती करते थे। वक्त गुजरने के साथ ही ये खेत बंजर पड़ते चले गए। कुछ खेतों में आईटीबीपी के जवान वक्त काटने के लिए आलू उगा लेते हैं। इससे उनका मन भी लगा रहता है और ताजा खाना भी मिल जाता है।

मिलम गांव के ज्यादातर परिवार अब बाहर बस गए हैं। मिलवाल, रावत, पांगती, धर्मशक्तु, निखुरपा, नित्वाल, धमोत के वंशज मिलम को सदियों पहले पीछे छोड़कर देशभर में फैल गए हैं। ग्रीष्मकालीन प्रवास पर अब यहां बहुत कम परिवार लौटते हैं। जोहार के बारह गांवों के हालात अब मेहमानदारी लायक भी नहीं रहे हैं। कई मकानों की सिर्फ दीवारें ही बची हुई हैं। इन खंडहर हो चुके मकानों के अंदर अब खेती होती है। प्रवास पर आने वालों ने दूर गोरी किनारे के खेतों को आबाद करने के बजाय एक बेहतरीन उपाय निकाल खंडहर हो चुके मकानों के अंदर ही जड़ी-बूटी और मौसमी सब्जियां उगाने के लिए क्यारियां बना ली हैं।
1962 से पहले जब तक भारत का तिब्बत के साथ व्यापार चलता था, इन गांवों की चहल-पहल देखने लायक होती थी। बुजुर्ग बताते हैं कि मानसरोवर जाने के लिए ये मार्ग छोटा है, लेकिन दर्रों की वजह से कई कठिनाइयां आती हैं। पश्चिमी तिब्बत की सबसे बड़ी मंडी ग्यानिमा, जो खार्काे के नाम से भी पहचानी जाती थी, यहां से कुल 105 किमी की पैदल दूरी पर है। तब के जमाने में जुलाई व अगस्त के महीनों में इस मार्ग से व्यापारियों का कारवां चलता रहता था। याक और भेड़ों पद लदे सामान के साथ टोलियां चल रही होती थी, लेकिन अब ये पड़ाव उजड़ा हुआ लगता है।
अंधेरा घिरने लगा तो हम वापस गुजरे हुए वक्त की गप्पें मारते हुए गांव के अपने ठिकाने पर चले आए। इस बार पांच परिवार ही मिलम में वापस प्रवास पर लौटे थे। पहले मुनस्यारी के ल्वां, बिल्जू, टोला, मिलम, मर्ताेली, बुर्फु, मापा, रेलकोट, छिलास आदि गांवों के हजारों सीमांतवासी अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बसे अपने गांवों में लौट आते थे। गांव वापस गुलजार होते थे। लोग तब उजड़े नहीं थे। वो गर्मियों में अपने खेतों को वापस आबाद करते थे। अपने आंगन बुहारते थे और अपने देवताओं के सम्मान में आयोजन करते थे। ये एक तरह के उत्सव होते थे। उनके खेतों में आलू, जम्बू, पल्थी, कालाजीरा जैसी कई महत्वपूर्ण फसलें उगती थी। जानवरों का चुगान बुग्यालों से हो जाता था।

फसल और जानवर ही इनकी आर्थिकी का एक प्रमुख साधन होते थे। इन्हीं से उनके परिवार की गुजर-बसर अच्छे ढंग से हो जाती थी, लेकिन अब संसाधनों के अभाव के साथ ही इस दुरूह क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को देखकर कम ही लोग जोहार में लौटते हैं। जोहार की समृद्धि को मैदानों की नजर लग गई... वो उजड़ी हुई बूढ़ी और जर्जर नजर आती है। घाटी के गांवों में वीरानी और सूख चुकी जड़ों की कहानियां तो हैं, लेकिन व्यापारियों से लकदक चमक नहीं। हिमालय के इस हिस्से ने खुद ही अपने आप को उजाड़ लिया है।



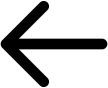 Previous
Previous






.%5B1%5D.jpg)









Leave your comment